लोकनाट्यों की सार्थकता: गोविन्द यादव
लोकनाट्य को पारम्परिक, परम्पराशील,
लोकधर्मी
नाट्य, जननाट्य,
क्षेत्रीय
या प्रादेशिक, ग्रामीण नाट्य अथवा आंचलिक
नाट्य आदि कई नामों से अभिहित किया जाता रहा है। कभी-कभी तो लोकगाथा और लोकनृत्य
को भी लोकनाट्य से संज्ञापित कर भ्रम पैदा की जाती है। हमें यह ज्ञात है कि लोक
में या लिखित साहित्य की परम्परा में किसी भी विधा की उपस्थिति की आवश्यकता और
अर्थ है। लोकगाथा, लोकनृत्य और लोकनाट्य
इसीलिए है कि समाज को इन तीनों की अलग-अलग आवश्यकता है। भिन्न-भिन्न कारणों से
समाज में इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। इन अनिवार्यताओं को समझते हुए,
इनकी
स्वतंत्रा, पहचान और नामकरण भी अति आवश्यक
है। यहाँ हम सिर्फ़ लोकनाट्य पर विमर्श करेंगे। लोकनाट्य सामासिक पद है,
जिसके
सामान्यतः दो अर्थ निकाले जा सकते हैं- लोक का नाट्य और लोक के लिए नाट्य।
संस्कृत
व्याकरण के अनुसार ‘लोक‘
शब्द
की उत्पत्ति संस्कृत की ‘लोक
दर्शने’ धातु में ‘घत्र‘
प्रत्यय
जुडने से हुई है, जिसका अर्थ है देखना।
इस तरह लोक शब्द का मूल अर्थ देखने वाला है। श्रीमदभागवत गीता में प्रयुक्त लोक
समूह शब्द का अर्थ भी जनसाधारण के आचरण तथा आदर्श से है। आचार्य हजारीप्रसाद
द्विवेदी ”लोक शब्द का अर्थ नगरों और
गाँवो की उस जनता को मानते है जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नही है। और
ये लोग सरल और कृत्रिम जीवन से अभ्यस्त होते हुए परिष्कृत सभ्य लोगों की समूची
विलासिता, सुकुमारता के लिए आवश्यक
वस्तुएँ उत्पन्न करते है“।१
स्पष्ट है कि ”लोक कि अभिव्यक्ति में जीवन के
जो तत्व है वे हमारे साहित्य के विकास के अवरुद्ध मार्ग को नई गति प्रदान करते है।
उसे संवर्धित और संप्रेषित करने में अहम भूमिका का निर्वाह करते है“।२
निष्कर्ष
यह है लोक समाज का वह वर्ग है जो अभिजात संस्कार, शास्त्रीयता,
पांडित्य
की चेतना और उसके अहंकार से मुक्त है जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित है। लोक
किसी भी राष्ट्र का जन समुदाय है, वह
नगर, गाँव कहीं भी रह सकता है यदि उनका ज्ञान या
कला- वर्षों से परम्परित और अनुभवजन्य है तथा मौखिक परम्परा में है तो वह लोकज्ञान
या लोककला कहा जाएँगे।
नाट्य
पुरुषवाचक संस्कृत का शब्द है। वर्तमान समय में थिएटर, नाट्य
का पर्याय माना जाता है। भारतीय नाट्य लक्षणग्रंथों में ‘नाट्य’
की
व्याख्या के संदर्भ में बार- बार नृत्त और नृत्य शब्द की चर्चा होती है। डॉ
कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार ”लोकनाट्य
में गीत, नृत्य और संगीत की त्रिवेणी
प्रभावित होती है। इन तीनों के माध्यम से समान्य जन अपने विचारों,
भावनाओं
को अभिव्यक्त करता है“।३ लोकनाट्यों के गद्य
संवाद-गीत न होकर, संवाद गीत है,
जो
लयबद्ध गद्य जैसा है। जाहिर है कि ऐसे संवाद नाट्यगत चरित्रों के होते हैं। नृत्य,
दृश्य
विधा है, जबकि नाट्य को दृश्य और श्रव्य
दोनों कहा गया है। इस प्रकार लोकनाट्यों के संदर्भ में लोक साहित्यक विद्वानों के
विचार निम्नवत है।”लोकनाट्य लोक जीवन के
सार गर्भित भाव से सम्पन्न। तत्कालीन युग की प्रवृत्ति का मौलिक आख्यान करता है।
जीवन में किसी भी परिस्थिति में एक रस हो कर कोई भी जीवित नही रह सकता है। लोक
मानस ने अपनी प्रवृत्ति को मनोरंजन प्रदान करने के लिए नए-नए आयामों की व्यवस्था
की। कालांतर में यही साहित्यिक विधाओं के रूप में विकसित हुए“।४
यदि हम लोकनाट्यों के संदर्भ में देखे तो लोकनाट्य कहलाने के लिए निम्नलिखित
तत्वों का होना अनिवार्य होगा।
नाट्यलेख
मौखिक परंपरा में तथा लेखक अज्ञात होता है। अभिनेता संवाद या गीत याद नहीं करेंगे,
बल्कि
घटनाओं पर तत्काल आशुचरन करेंगे। मंच व्यवस्था अनौपचारिक होगी,
अभिनेता
कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अभिनय या प्रदर्शन कर अंचल विशेष के लोकधुनों और
नृत्यों का समुचित प्रयोग करेगा और पारम्परिकता का निर्वाह।
परम्परा
पारम्परिकता
का निर्वाह लोक का प्रथम और आवश्यक गुण है। परम्परा से तात्पर्य है वह जो वर्षों
से प्रचलित हो तथा परिवर्तनशील होते हुए भी चिरंजीवी हो। ‘मानव
हिन्दी कोश’ में परम्परा के सम्बन्ध में
निम्नलिखित बातें कही गई हैं। वह व्यवहार जिसमें पुत्र, पिता
की, वंशज, पूर्वजांे
की और नई पीढ़ी वाले पुराने पीढ़ी वालों की देखा-देखी उनके रीति-रिवाज़ों का अनुकरण
करते हैं। वह रीति-रिवाज़ जो बड़ों, पूर्वजों
या पुरानी पीढ़ी उनके रीति रिवाज़ों का अनुकरण करते हैं। नियम या विधान से भिन्न
अथवा अनुलिखित वह कार्य जो बहुत दिनों से एक ही रूप में होता चला आ रहा है और
इसलिए जो सर्वमान्य हो। (मानव हिन्दी कोश, खण्ड,
3, पृ. 396)
भारतीय
लोक की विशेषता है चिरनवीनता और यह परम्पराधर्मी होने के कारण ही संभव है। परम्परा
की चेतन सत्ता के आधार पर नित नए प्रयोग, नए
मूल्य तथा धारणाएँ कायम की जा सकती है। इस प्रकार परम्परा की छाप प्रत्येक युग में
अभिव्यक्ति के पीछे रहती है। प्रत्येक युग में परम्परा को अपनाकर नए प्रयोग किए
जाते रहे हैं। ”लोक परंपरा मनुष्य व प्रकृति
के बीच में व्यक्त व अव्यक्त के बीच मे संबंध स्थापित करती है“।५
कहने का अर्थ है कि हम अतीत से बंधे तो अवश्य हैं, परन्तु
परम्परा का यह अर्थ नहीं है कि हम उसे ढोते चलें। परम्परा तभी जीवन्त होगी जब हम
वर्तमान के साथ उसका समन्वय करें, उसमें
नए प्रयोग करें। और यही प्रयोग प्रत्येक युग से अपना समन्वय स्थापित कर उस युग के
अनुकूल एवं लोक बन जाता है और अनंत काल के लिए जीवित भी। जो परम्परा परिवर्तन का
आकांक्षी नहीं होगी या परम्परा में परिवर्तन की लचक नहीं होगी,
तो
वह अवरूद्ध होगी और मर जाएगी। इस तरह परम्पराशीलता लोक का प्रथम और आवश्यक गुण है।
”लोक परंपरा भारत वर्ष में शास्त्र को
समृद्ध करने वाली और श्रेष्ठ की अपेक्षा श्रेष्ठतर परंपरा रही है“।६
अतः जो लोक है, पारम्परिक भी है। अतः
लोकनाट्यों को पारम्परिक नाट्य कहना समीचीन है।”लोकनाट्य
परंपरा का इतिहास उसके नैरंतर्य मे ही प्रकट होता है। अन्यथा उसके पहचान चिन्हों
और उसकी प्रस्तुतियों का लेखा जोखा कही नही रखा गया है“।७
”सर्वसाधारण
का मनोरंजन और नीति तथा धर्म का उपदेश, ये
दो लक्षण जो भरत मुनि ने पंचम वेद के लिए स्थिर किए थे, संस्कृत
की नाट्य धारा में प्रतिबिम्बित नही हुए“।८ 10
वीं से 12 वीं शताब्दी तक संस्कृत की
प्रधान नाट्यधारा कुछ क्षीण हो गयी थी। धीरे- धीरे जनसाधारण के मानस से मनोरंजन और
शिक्षा से अनुप्राणित विभिन्न शैलियों का उदय होने लगा। इन नाट्य प्रदर्शन के
उभरने का कारण राजाओं, महाराजाओं पर कम आश्रित
होना, लक्षणकारों के सिद्धांतों की
उपेक्षा, धार्मिक स्थानों,
मेलों
और उत्सवों में लोक मनोरंजन करके, विभिन्न
कलाओं का समावेश, आदि है।
संस्कृत
नाट्य परम्परा के प्रतिफलन में निश्चित रूप से तत्कालीन या उससे पूर्व प्रचलित लोक
परम्पराओं का योगदान रहा होगा। संस्कृत नाट्य के श्रेण्य युग में रसिकों की
अभिरुचि के दबाव के कारण तत्कालीन नाट्य प्रयोक्ताओं ने एक ऐसी नाट्य पद्धति को
विकसित किया जिसमें संगीत और नृत्य का प्राचुर्य था। इस अभिनव नाट्य रूप को संगीतक
कहा गया। ”संगीतक का सर्वप्रथम उल्लेख
वररुचि के उभयासारिका नामक चतुर्भाणी में हुआ है। बाणभट्ट के कादम्बरी में भी
चतुर्भाणी का उल्लेख मिलता है। सातवीं शताब्दी तक इस गौण उपरूपक ने संगीत-नाटक या
संगीतक के रूप में अपनी पहचान बना ली थी“।९
कालान्तर में इस नाट्यरूप ने भाषा संगीतक (किरतनि´ायां
और अंकिया) के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। जहाँ राजदरबारों में नाट्यकला
को प्रोत्साहन और संरक्षण मिलता रहा वहीं भक्ति आन्दोलन ने नाट्यकला को
महत्त्वपूर्ण सामाजिक चेतना के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया। इस काल में
उद्भित अधिकांश नाट्यरूपों का गहरा सामाजिक सरोकार था।”चैदहवीं
शताब्दी में मिथिला में कर्णाटवंशी शासक हरिहर सिंह देव ने नाट्यकलाओं और
नाटककारों को प्रश्रय दिया। उनके ही दरबार में ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने धूत्र्तसमागम
और उमापति ने पारिजातहरण नाटक की रचना की“।१॰
पन्द्रहर्वी शताब्दी तक भक्ति आन्दोलन का प्रसार उत्तर और पूर्व भारत में हो चुका
था। ब्रजमंडल देश के वैष्णव भक्तों का केन्द्र बना। किरतनि´ायां,
अंकिया
और जात्रा पर वैष्णव धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार भारतीय लोकनाट्य
की परंपरा प्राचीन रही है देश काल के साथ-साथ लोकनाट्य के कथनांक और मंचन शैली के
स्वरूप में निरंतर परिवर्तन आया है। परिवर्तन का कारण समृद्ध भारतीय संस्कृति,
बहुभाषा
समाज, भक्ति आन्दोलन और राष्ट्रीय
चेतना रही है। आगे लोक नाट्य की सार्थकता को निम्न प्रकार से समझ सकते है।
लोकनाट्य
की भाषा सरल और सीधी सदी होती है। लोकनाट्य पर क्षेत्र विशेष की (रिजनल डाइलेक्ट)
का प्रभाव परिलक्षित होता है। भाषा अलंकृत नहीं होकर दैनिक प्रयोग में व्यवहारिक
होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश व ब्रज की रासलीला में कथनांक में परिवर्तन न होकर
क्रमशः भोजपुरी और ब्रज बोली का प्रयोग किया जाता है। लोकनाट्य के संवाद छोटे और
सरल होते है। व्यवाहरिक समस्याओं, मनोरंजन
आदि से जुडे होने के कारण संवाद को जनसाधारण सरलता से आत्मबोध कर लेता है। मुख्यतः
संवाद प्रश्नोत्तरीय होते है। कभी-कभी प्रश्नोत्तर दो-तीन शब्दों तक ही सीमित होता
है। कथनांक ऐतिहासिक, पौराणिक,
धार्मिक,
सामाजिक
अथवा संस्कृतिक होते है। जैसे- केरल के यक्षगान लोकनाट्य पौराणिक है। जात्रा और
किरतनिया धार्मिक लोकनाट्य है। विषय वस्तु धार्मिक, पौराणिक,
ऐतिहासिक
होने पर भी समकालीन समस्याओं और मनोरंजन के तत्वों का समावेश दर्शकों को बाधे रखता
है।
लोकनाट्य
की मंच सज्जा मूलतः खुले प्रांगण में होती है। काठ के तख्तों का मंच बना लिया जाता
है। रंगमंच पर पर्दों का उपयोग नहीं होता है। दर्शक मंच के चारों और बैठ सकते है।
लोकनाट्य में मुख्यतः पुरुष पात्र ही अभिनय करते है। लोकनाट्य में अभिनय,
नृत्य,
गायन
तीनों का समावेश होता है। अतः लोकनाट्य को लोकनृत्य नाट्य कहना युक्ति संगत होगा।
आधुनिक
परिप्रेक्ष्य में, ”लोकनाट्य और लोक मंच
हमारी प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और परंपरागत
रूढियों में वर्णित जीवन पद्धति, जीवन
प्रकृति और प्रवृत्ति के स्वरूप को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हूए है। अपने
वर्तमान युग के लोक मानस का दशा-दिशा ज्ञान कराते हुए अपने युग धर्म के प्रति
प्रतिबद्ध हैं“।११ पारंपरिक होते हुए भी
लोकनाट्य शैलियों में लचीलापन हैं। सांग, नौटंकी,
ख्याल,
कूडियट्टम,
आदि
में कथानकों अथवा प्रसंगों द्वारा वर्तमान समस्याओं का समावेश होता रहता है। जिससे
इनकी प्रासंगिकता और जीवंतता बनी रहती है। “लोकनाट्य
का अपना निजी अनुशासन है। लोकनाट्य का रचना विधान, निरंतर
प्रयोग और लोक चेतना के परस्पर आदान- प्रदान और आवश्यकताओं से रूपायित हुआ है।
उनकी आंतरिक रचना प्रक्रिया के सूत्र नितांत भिन्न है।”१२
जिन लोक नाट्य को हम देखते है या कभी कभी देखने का अवसर मिलता है,
उन्हें
हम मूल रूप में नहीं देख पाते है। परंपराशील होते हुए भी उनमें परिवर्तन होते रहते
है। लोकनाट्यों में रचयिता, पात्र,
दर्शक
और व्यवस्थापकों के बीच भेद नहीं होता है। यही कारण हैं कि इनका दर्शक फैशन के लिए
इन्हे नहीं देखता है, उसके अलगाव में संस्कार
जन्य मनोरंजन का लक्ष्य स्पष्ट है। “लोकनाट्य
कि सार्थकता का ही प्रमाण है कि लोकनाट्यों ने अपने स्वरूप और निजी क्षेत्र के
दर्शकों के बीच आत्मीय संबंध कायम रखा है। नाटकों से संबन्धित सभी बाते दर्शकों कि
जानकारी में होती है।”१3
बापुजी कि पड़ दिखाने वाले भोपे प्राचीन कथाएँ कहते है और उन्हें व्यक्त करने वाली
शैलियाँ आज भी लोकजन को बाधे रखती है। ऐसे लोकनाट्य जिनमें वर्तमान जीवन के साथ
बने रहने कि क्षमता है। वे स्वंय नवीन परिस्थियों में अपना अस्तित्व सार्थक कर
लेती है। लोकनाट्य का क्षेत्रीय महत्व नष्ट नही हुआ है। रामलीला और रासलीला
लोकनाट्य में परिवर्तन हुए हैं, लेकिन
कथा कि रूपरेखा और संवेदना के बिन्दु नही बदले है। दर्शक आज भी वर्तमान स्वरूप को
उतना ही पसंद करते है जितना पहले करते थे।
भारतीय
संस्कृति में स्थित विभिन्न कलाओं में से लोकनाट्य संस्कृति के विकास का सशक्त
मध्यम है। लोकनाट्य दर्शकों के मन जीवन के विभिन्न रूपों को स्थापित,
विचित्रताओं
को उन्मीलित, शंगार विषाद,
विरह
आदि रसों की सृष्टि कर हृदयावेग को प्रबुद्ध करता है। बिहार के लोकनाट्य राजा
सलहेस और रेशमा चुहड़मल वीरता के साथ- साथ वर्ग संघर्ष, सामंती
व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध, स्त्री
अस्मिता के प्रश्न, और धार्मिक आडंबरों पर
प्रहार करता है। उक्त सभी समस्याएँ बारहवीं शताब्दी में थी और वर्तमान समाज में
अनेक रूपों में बनी हुई है। इसलिए दोनों लोकनाट्य की सार्थकता बढ़ जाती है। “प्रतिरोधी
संघर्ष के अतिरिक्त लोकनाट्य में लोक जीवन की सरलता, स्पष्टता,
माधुर्य,
स्थानीयता,
आदि
अनेक विशिष्टताएँ परिलक्षित होती है। लोकनाटक के निकष पर किसान,
मजदूर
वर्ग, अर्थात निम्न और मध्म वर्ग की
सामूहिक ऊर्जा और बौद्धिक गहराई मापी जा सकती है।”१४
लोकनाट्य के दृश्य, श्रव्य होने के कारण
जनसाधारण और सभ्य समाज से सतत आदान-प्रदान होता रहता है। समाज में स्थित गुण अवगुण,
रीति
कुरीति दोनों को लेकर अपनी कलात्मक क्षमता से दर्शकों तक पहुंचाता है। धार्मिक
जीवन के साथ-साथ सामाजिक पक्ष भी सामने आता है। अनेक लोकनाट्य में समाज में फैली
विभिन्न समस्याओं यथा, बाल विवाह,
बेमेल
विवाह, दहेज प्रथा,
ग्रामीणों
पर हो रहे अत्याचार, गाँव छोड़कर शहर की तरफ
पलायन, आदि को मनोरंजन के तत्वों के
साथ मंचित कर समाज को मार्ग दर्शित किया जाता है। भिखारी ठाकुर के सभी नाटक,
मैथली
के जट-जटिन, लोरिकयान,
उत्तरप्रदेश
की नौटंकी, महाराष्ट्र का तमाशा,
राजस्थान
की कठपुतली आदि सभी में इन समस्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। वर्तमान समय में
इन समस्याओं को हम नकार नही सकते है। इसलिए लोकनाटकों की प्रासंगिकता आज भी बनी
हुई है। लोकनाट्य जीवन के विविध अनुभवों, जनजीवन
की विकृतियों, कमजोरियों,
ऊँच-
नीच, रिश्वत खोरी, व्यभिचार,
भ्रष्टाचार,
छुआछूत
की भावना, शोषण, उत्पीड़न
आदि भावों को मंच पर उजागर करता है। और दर्शकों को हँसाता रुलाता,
और
प्रफुल्लित करता है। लोकनाट्य के कलाकार गायन, नृत्य,
अभिनय
भी करते है और दर्शकों का मन जीत लेते है। सामुदायिक धर्म के प्रति जन भावना,
भंगिमा
तथा रवैये की बदौलत ही लोकनाट्य की निर्मिति होती है तथा इसका लक्ष्य भी इनका पोषण
करने का होता है। यही वजह है कि तमाम लोकनाटक मिथक में अधिक रचे बसे है।१५
लोकनाट्य
कि सार्थकता का जीवंत उदाहरण दिल्ली में हो रहे 18
वें भारतीय रंग महोत्सव से लगाया जा सकता है। जिसमें 2
फरवरी को मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय के कन्हैयालाल कैथवास ने ’अग्निवर्षम’
नाटक
को गोंडवानी, भाषा में प्रस्तुत किया।
मध्यप्रदेश के पारंपरिक गीतों के साथ लोकनाट्य नाचा कि शैली और नृत्य का समवेश
किया गया। नाटक महकौशल के आस-पास बुना गया था। जिसमें, पंडवानी,
गोंडवानी
और रामायणी का प्रयोग किया गया। भोपाल से आये रंगाश्री लिटिल नृत्य नाटक समूह ने
रामायण का मंचन किया। इसमें सभी कलाकारों ने लकड़ी का मौखटा पहनकर कठपुतली के रूप
में राजस्थान कि पुतुल नाट्य शैली में मंचन किया। 4
फरवरी को नौटंकी का प्रदर्शन किया गया। जिसमें निर्देशक छ्ज्जन सिंह ने अमर सिंह
राठौर के राष्ट्रप्रेम और गोने कि प्रथा को दर्शाया है। 10
फरवरी को तमिल निर्देशक कलाईमनी पी॰ के॰ संबंधन ने महाभारत कि कथा ’द्रौपदी
वस्त्रापरणम््’ को लोकनाट्य तेरुकुट्टू शैली
में प्रस्तुत किया। 2015 में
भारतीय रंग महोत्सव में संस्कृत के नाटक कर्णभारम की प्रस्तुति सीधी के युवा
निर्देशक नीरज कुंदेर ने बघेली क्षेत्र के लोकनाट्य शैली में की। बघेली बोली और
वस्त्र विन्यास को दर्शको ने खूब सराह था। ये सभी मंचन लोकनाट्य के बढ़ते प्रभाव और
सार्थकता को प्रमाणित करते है।
रंगनिर्देशक,
शोधार्थी
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मंचन की शैलियों, भाषाओं
में अनुसंधान कर और प्रकाशन की योजना बना कर साहित्य चिंतकों के समक्ष प्रस्तुत
करें, जिससे हमारी संस्कृति,
सभ्यता
और जीवन के लौकिक पक्षों को साहित्य जगत के सामने लाया जा सकेगा। इससे भारतीय जीवन
और साहित्य को एक नई रश्मि मिलेगी साथ ही भारतीय समाज को समझने की दिशा। नेमिचंद
जैन का मत है कि ”हमारे रंग जीवन का एक
अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है लोकनाट्य, जो
रंगकर्मियों से बडी संवेदनशीलता, सर्जनात्मक
दृष्टि और प्रामाणिकता कि मांग करता है। लोकनाट्य हमारी नाट्य परंपरा की मूल-भूत
कड़ी है, क्योंकि वह अनेक प्रकारों और
रूपों में संस्कृत नाटक के बाद मध्यकालीन नाट्य परंपरा का ही निरंतरण है अनेक दृष्टियों से उसमें संस्कृत रंगमंच से कहीं
अधिक विविधिता है“।१६
लोकनाट्यों
को आधुनिक नाटकों की तरह इलेक्ट्रोनिक मीडिया के सहयोग से मंच पर उपस्थित किया
जाए। लोकनाट्य शैली को लेकर पिछले कुछ समय से आधुनिक नाटकों और सिनेमा में प्रयोग
होने लगे है। स्पष्ट है भारतीय लोक नाटकों के विकास का बीज लोकनाट्यों में निहित
है। गंभीर नाट्यनुरागी लोकनाट्य की अपेक्षा कर आगे नही बढ़ सकते है।
संदर्भ
ग्रंथ
1. डॉ‐ हजारी
प्रसाद द्विवेदी, विचार और वितर्क,
जनपद
अंक 1, पृ॰ 65
2. प्रेम शंकर सिंह,
मैथली
लोक नाट्य, समकालीन भारतीय साहित्य,
जुलाई-
अगस्त 2002, पृ॰135
3. डॉ‐ कृष्णदेव
उपाध्याय, लोक साहित्य की भूमिका,
साहित्य
भवन, इलाहाबाद 1957,
पृ॰
83
4. प्रेम शंकर सिंह,
मैथली
लोक नाट्य, समकालीन भारतीय साहित्य,
जुलाई-अगस्त
2002 पृ॰ 136
5. विद्यानिवास मिश्र,
लोक
और लोक का स्वर, प्रभात प्रकाशन 2000,
पृ॰35
6. वही, पृ
-36
7. श्याम सुंदर दुबे,
लोकः
परंपरा, पहचान एवं प्रवाह,
राधाकृष्ण
प्रकाशन, 2003 पृ॰ 33
8. जगदीशचन्द्र माथुर,
परंपराशील
नाट्य, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद,
पटना
2000, पृ॰ 4
9. वही, पृ॰
10-11
10. वही, पृ॰
19-20
11. प्रेम शंकर सिंह,
मैथली
लोकनाट्य, समकालीन भारतीय साहित्य,
जुलाई-
अगस्त 2002, पृ॰ 144
12. श्याम परमार,
लोक
साहित्य विमर्श, पृ॰ 222
13. वही, पृ॰
232
14. डॉ रेखा दास,
बिहार
के लोकनाटकों की प्रमुख शैलियों का विवेचन,
1994, पृ॰ 166
15. पीयूष दईया,
लोक,
भारतीय
लोक कला मण्डल 2002 पृ॰,
629
16‐
नेमिचन्द
जैन, रंग दर्शन, अक्षर
प्रकाशन, 1967, प्रथम संस्करण,
पृ॰
80
पीएच॰ डी॰ शोधार्थी
जामिया मिलिया इस्लामिया,
नई दिल्ली
मो॰ 9910773493
[जनकृति के अंक 23 में प्रकाशित शोध आलेख]










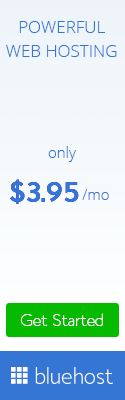




कोई टिप्पणी नहीं:
धन्यवाद