प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक साधन
प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति तथा शासन कला का अध्ययन करने के पूर्व इतिहास की
उन सामग्रियों का अध्ययन करना अत्यावश्यक है जिनके द्वारा हमें प्राचीन भारत के
इतिहास का ज्ञान होता है। यों तो भारत के प्राचीन साहित्य तथा दर्शन के संबंध में
जानकारी के अनेक साधन उपलब्ध हैं, परन्तु भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी के साधन
संतोषप्रद नहीं है। उनकी न्यूनता के कारण अति प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं शासन का
क्रमवद्ध इतिहास नहीं मिलता है। फिर भी ऐसे साधन उपलब्ध हैं जिनके अध्ययन एवं
सर्वेक्षण से हमें भारत की प्राचीनता की कहानी की जानकारी होती है। इन साधनों के
अध्ययन के बिना अतीत और वर्तमान भारत के निकट के संबध की जानकारी होती है। इन
साधनों के अध्ययन के बिना अतीत और वर्तमान भारत के निकट के संबंध की जानकारी करना
भी असंभव है।
प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधनों को दो भागों
में बाँटा जा सकता है-साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन, जो देशी और विदेशी दोनों हैं। साहित्यिक साधन दो प्रकार के
हैं-धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के
हैं-ब्राह्मण ग्रन्थ और अब्राह्मण ग्रन्थ। ब्राह्मण ग्रन्थ दो प्रकार के
हैं-श्रुति जिसमें वेद ब्राह्मण उपनिषद इत्यादि आते हैं और स्मृति जिसके अन्तर्गत
रामायण महाभारत पुराण स्मृतियाँ आदि आती हैं। लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के
हैं-ऐतिहासिक साहित्य विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य।
प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख साधन साहित्यिक
ग्रन्थ हैं जिन्हें दो उपखण्डों में रखा जा सकता है-धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इनका पृथक-पृथक उल्लेख करना आवश्यक
है।
ब्राह्मण ग्रन्थ प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्रदान करने में अत्यधिक
सहयोग देते हैं। भारत का प्राचीनतम साहित्य प्रधानतः धर्म-संबंधी ही है। ऐसे अनेक
ब्राह्मण ग्रन्थ हैं जिनके द्वारा प्राचीन भारत की सभ्यता तथा संस्कृति की कहानी
जानी जाती है। वे निम्नलिखित मुख्य हैं-
(क) वेद- ऐसे
ग्रन्थों में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं और वे सबसे पहले आते हैं। वेद आर्यों के
प्राचीनत ग्रन्थ हैं जो चार हैं-ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से आर्यों के प्रसार; पारस्परिक युद्ध; अनार्यों, दासों, दासों और दस्युओं से उनके निरंतर संघर्ष तथा उनके सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी
प्राप्त होती है। इसी प्रकार अथर्ववेद से तत्कालीन संस्कृति तथा विधाओं का ज्ञान
प्राप्त होता है।
(ख) ब्राह्मण-
वैदिक मन्त्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन
ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ,
पंचविश, तैतरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। ऐतरेय के अध्ययन से
राज्याभिषेक तथा अभिषिक्त नृपतियों के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। शथपथ के एक
सौ अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गान्धार, शाल्य तथा केकय आदि और प्राच्य देश, कुरु, पांचाल, कोशल तथा विदेह के संबंध में ऐतिहासिक कहानियाँ प्रस्तुत
करते हैं। राजा परीक्षित की कथा ब्राह्मणों द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पायी है।
(ग)
उपनिषद-उपनिषदों में ‘बृहदारण्यक’ तथा ‘छान्दोन्य’, सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन ग्रन्थों से बिम्बिसार के पूर्व
के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जनमेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं
उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का
दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। आर्यों के
आध्यात्मिक विकास प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिन्तन के जीते जागते जीवन्त उदाहरण
इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं।
(घ)
वेदांग-युगान्तर में वैदिक अध्ययन के लिए छः विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ
जिन्हें ‘वेदांग’ कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, तथापि इस साहित्य के पौरूषेय होने के कारण श्रुति साहित्य
से पृथक ही गिना जाता है। वे ये हैं-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, छन्दशास्त्र तथा ज्योतिष। वैदिक शाखाओं के अन्तर्गत ही उनका
पृथकृ-पृथक वर्ग स्थापित हुआ और इन्हीं वर्गों के पाठ्य ग्रन्थों के रूप में
सूत्रों का निर्माण हुआ। कल्पसूत्रों को चार भागों में विभाजित किया गया-श्रौत
सूत्र जिनका संबंध महायज्ञों से था, गृह्य सूत्र जो गृह संस्कारों पर प्रकाश डालते थे, धर्म सूत्र जिनका संबंध धर्म तथा धार्मिक नियमों से था, शुल्व सूत्र जो यज्ञ, हवन-कुण्ठ बेदी, नाम आदि से संबंधित थे। वेदांग से जहाँ एक ओर प्राचीन भारत
की धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, वहाँ दूसरी ओर इसकी सामाजिक अवस्था का भी।
(ङ) रामायणः
महाभारत—वैदिक साहित्य के उत्तर में रामायण और महाभारत नामक दो
महाकाव्य साहित्य का प्रणयन हुआ। सम्पूर्ण धार्मिक साहित्य में ये दोनों महाकाव्य
अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। रामायण की रचना महर्षि बाल्मीकि ने की जिसमें
अयोध्या की रामकथा है। इसमें राज्य सीमा, यवनों और शकों के नगर, शासन कार्य रामराज्य आदि का वर्णन है। मूल महाभारत का
प्रणयन व्यास मुनि ने किया। महाभारत का वर्तमान रूप प्राचीन इतिहास कथाओं उपदेशों
आदि का भण्डार है। इस ग्रन्थ से भारत की प्राचीन सामाजिक तथा धार्मिक अवस्थाओं पर
प्रकाश पड़ता है। इन दोनों महाकाव्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे आर्य
संस्कृति के दक्षिण में प्रसार का निर्देश करते हैं। रामायण में तत्कालीन पौर
जनपदों और महाभारत से ‘सुधमां’ और ‘देवसभा’ का हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे पता चलता है कि राजा किस सीमा तक स्वेच्छाचारी था और
कहां तक उसके प्रभाव और कार्य की सीमायें इन राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रजा
प्रतिनिधित्व द्वारा परिमित थी।
(च) पुराण-
महाकाव्यों के पश्चात् पुराण आते हैं जिनकी संख्या अठारह है। इनकी रचना का श्रेय ‘सूत’ लोमहर्षण अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवस या उग्रश्रवा को दिया जाता है। पुराणों
में पाँच प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धान्ततः इस प्रकार है-सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है प्रतिसर्ग प्रलय
के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं, वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है, मन्वन्तर में कल्प के महायुगों का वर्णन है जिनमें से
प्रत्येक में मनुष्य का पिता एक मनु होता है और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं
जिनमें राजवंशों की तालिकायें दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कथाओं और घटनाओं के वर्णन हैं। उपर्युक्त पांच पुराण के
विषय होते हुए भी अठारहों पुराणों में वंशानुचरित का प्रकरण प्राप्त नहीं होता। यह
दुर्भाग्य ही है क्योंकि पुराणों में जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण
विषय है,
वह वंशानुचरित है। वंशानुचरित केवल भविष्य, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्माण्ड तथा भागवत पुराणों में ही प्राप्त होता है।
गरुड़-पुराण में भी पौरव, इक्ष्वाकु और बार्हदय राजवंशों की तालिका प्राप्त होती है। पर इनकी तिथि
पूर्णतया अनिश्चित है। पुराणों की भविष्यवाणी शैली में कलियुग के नृपतियों की
तालिकाओं के साथ शिशुनाग, नन्द,
मौर्य, शुंग, कण्व, आन्ध्र तथा गुप्तवंशों की वंशावलियाँ भी प्राप्त होती हैं।
शिशुनागों में ही बिम्बिसार एवं अजातशत्रु का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार पुराण चौथी शताब्दी की
स्थितियों का उल्लेख करते हैं। मौर्य वंश के संबंध में विष्णु पुराण में अधिक
उल्लेख मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार मत्स्य पुराण में मान्ध्र वंश का पूरा उल्लेख
मिलता है। वायु पुराण गुप्त सम्राटों की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालते हैं। इन
पुराणों में शूद्रों और म्लेच्छों की वंशावली भी दी गयी है। आभीर, शक, गर्दभ, यवन, तुषार, हूण आदि के उल्लेख इन्हीं सूचियों में मिलते हैं।
(छ) स्मृतियाँ–ब्राह्मण ग्रन्थों में स्मृतियों का भी ऐतिहासिक महत्व है।
मनु,
विष्णु, याज्ञवल्क्य नारद, वृहस्पति, पराशर आदि की स्मृतियाँ प्रसिद्ध हैं जो धर्म शास्त्र के
रूप में स्वीकार की जाती हैं। मनुस्मृति में जिसकी रचना संभवतः दूसरी शताब्दी में
की गयी है, धार्मिक
तथा सामाजिक अवस्थाओं का पता चलता है। नारद तथा वहस्पति स्मृतियों से जिनकी रचना
करीब छठी सदी ई. के आस-पास हुई थी, राजा और प्रजा के बीच होने वाले उचित संबंधों और विधियों के
विषय में जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त पराशर, अत्रि हरिस, उशनस, अंगिरस, यम, उमव्रत, कात्यान, व्यास, दक्ष, शरतातय, गार्गेय वगैरह की स्मृतियाँ भी प्राचीन भारत की सामाजिक और
धार्मिक अवस्थाओं के बारे में बतलाती हैं।
धार्मिक साहित्य के ब्राह्मण ग्रन्थों के अतिरिक्त अब्राह्मण ग्रन्थों से उस
समय की विभिन्न अवस्थाओं का पता चलता है।
(क) बौद्ध
ग्रन्थ-बौद्धमतावल्बियों ने जिस साहित्य का सृजन किया, उसमें भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए प्रचुर सामग्रियाँ
निहित हैं। ‘त्रिपिटक’ इनका महान ग्रन्थ है। सुत, विनय तथा अमिधम्म मिलाकर ‘त्रिपिटक’ कहलाते हैं। बौद्ध संघ, मिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के लिये आचरणीय नियम विधान विनय
पिटक में प्राप्त होते हैं। सुत्त पिटक में बुद्धदेव के धर्मोपदेश हैं। गौतम
निकायों में विभक्त हैं-
प्रथम दीर्घ निकाय में बुद्ध के जीवन से संबद्ध एवं उनके
सम्पर्क में आये व्यक्तियों के विशेष विवरण हैं। दूसरे संयुक्त निकाय में छठी
शताब्दी पूर्व के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है, किंतु सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी इससे अधिक होती
है। तीसरे मझिम निकाय को भगवान बुद्ध को दैविक शक्तियों से युक्त एक विलक्षण
व्यक्ति मानता है।
चौथे, अंगुत्तर निकाय में सोलह महानपदों की सूची मिलती हैं।
पाँचवें,
खुद्दक निकाय लघु ग्रंथों का संग्रह है जो छठी शताब्दी ई.
पूर्व से लेकर मौर्य काल तक का इतिहास प्रस्तुत करता है। अमिधम्म पिटक में बौद्ध
धर्म के दार्शनिक सिद्धान्त हैं। कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी हैं। मिलिंदमन्ह में
यूनानी शाशक मिनेण्डर और बौद्ध मिक्षु नागसेन के वार्तालाप का उल्लेख है।
‘दीपवंश’ मौर्य काल के इतिहास की जानकारी देता है। ‘महावंश’ भी मौर्यकालीन इतिहास को बतलाता है। ‘महाबोधिवंश’ मौर्य काल का ही इतिहास माना जाता है। ‘महावस्तु’ में भगवान बुद्ध के
जीवन को बिन्दु बनाकर छठी शताब्दी ई. पूर्व के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। ‘ललित विस्तार’ में बुद्ध की ऐहिक लीलाओं का वर्णन है जो महायान से संबद्ध
है। पाली की ‘निदान
कथा’
बोधि सत्वों का वर्णन करती है। यातिमोक्ख, महावग्ग, चुग्लवग्ग, सुत विभंग एवं परिवार में भिक्खु-भिक्खुनियों के नियमों का
उल्लेख है। ये पाँचों ग्रन्थ ‘विनय’
के अन्तर्गत आते हैं।
अमिधम्म के सात संग्रह है जिनमें तत्वज्ञान की चर्चा की गयी है। ऐतिहासिक
ज्ञान के लिए त्रिपिटकों का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि इसमें बौद्ध संघों के
संगठनों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार बौद्धग्रन्थों में जातक कथाओं का दूसरा
महत्वपूर्ण स्थान है जिनकी संख्या 549 है। ‘‘इनका महत्व केवल इसीलिए नहीं है कि उनका साहित्य और कला
श्रेष्ठ है, प्रत्युत
तीसरी शताब्दी ई. पूर्व की सभ्यता के इतिहास की दृष्टि से भी उनका वैसा ऊँचा मान
है।’’
जातक में भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथाएँ उल्लिखित
हैं।
(ख) जैन ग्रन्थ- प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त
करने के लिए जैन ग्रन्थ भी उपयोगी हैं। ये प्रधानतः धार्मिक हैं। इन ग्रन्थों में ‘परिशिष्ट पर्वत’ विशेष महत्वपूर्ण हैं। ‘भद्रबाहु चरित्र’ दूसरा प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ है जिसमें जैनाचार्य भद्रबाहु के
साथ-साथ चन्द्रगुप्त मौर्य के संबंध में
भी उल्लेख मिलता है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त कथा-कोष, पुण्याश्रव-कथाकोष, त्रिलोक प्रज्ञस्ति, आवश्यक सूत्र, कालिका पुराण, कल्प सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र आदि अनेक जैन ग्रन्थ भारतीय इतिहास की
सामग्रियां प्रस्तुत करते हैं। इनके अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मिलन्दिपन्हो, दिव्यावदान
आदि ग्रन्थ की इन दोनों धर्मों तथा मौर्य साम्राज्य के संबंध में यत्र-तत्र उल्लेख
करते हैं।
Ø लौकिक साहित्य
ऐतिहासिक सामग्रियों की उपलब्धि के दृष्टिकोण से लौकिक साहित्य को प्रमुखतः
निम्न भागों में बाँटा जा सकता है-
(क) ऐतिहासिक ग्रन्थः ऐसे अनेक विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है
जिनमें केवल सम्राट तथा शासन से संबंधित तथ्यों का ही उल्लेख किया गया है। ऐसे
ग्रन्थों में कल्हण कृत ‘राजतरंगिणी’ नामक ग्रन्थ सर्वप्रथम आता है जो पूर्णतः ऐतिहासिक है।
इसमें कथा-वाहिक रूप में प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों राज्य शासकों और प्रशस्तियों
के आधार पर ऐतिहासिक वृतान्त प्रस्तुत किये गये हैं। इसकी रचना। 1148 ई. में प्रारम्भ की गयी थी। कश्मीर के सारे नरेशों के
इतिहास जानकारी इस प्रसिद्ध ग्रन्थ से होती है। इसमें क्रमबद्धता का पूरी तरह
निर्वाह किया गया है। इसी श्रेणी में तमिल ग्रन्थ भी आते हैं। ये हैं नन्दिवक
लाम्बकम्,
ओट्टक्तूतन का कुलोत्तुंगज- पिललैत्त मिल, जय गोण्डार का कलिंगत्तुंधरणि, राज-राज-शौलन-उला और चोलवंश चरितम्। इसी श्रेणी में सिंहल
के दो ग्रन्थ-दीपवंश और महावंश भी आते हैं जिनमें बौद्ध भारत का उल्लेख मिलता है।
गुप्तकालीन विशाखदत्त का ‘मुद्राराक्षस’ सिकन्दर के आक्रमण के शीघ्र बाद ही भारतीय राजनीति का
उद्घाटन करता है। पोरस, जिसने सिकन्दर के दाँत खट्टे कर दिये थे। मुद्राराक्षस के प्रमुख पात्रों में
एक है। साथ ही साथ, चन्द्रगुप्त मौर्य चाणक्य तथा कुछ तत्कालीन नृपतियों का भी इसमें उल्लेख मिलता
है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इस संबंध में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है जिसकी रचना
मुद्राराक्षस के पूर्व ही की गयी थी। इस ग्रन्थ में रचनाकार ने तत्कालीन
शासन-पद्धति पर प्रकाश डाला है। राजा के कर्त्तव्य, शासन-व्यवस्था, न्याय आदि अनेक विषयों के संबंध में कौटिल्य ने प्रकाश डाला
है। वास्तव में मौर्यकालीन इतिहास का यह ग्रन्थ एक दर्पण है।
पाणिनी का ‘अष्टाध्यायी’ एक व्याकरण ग्रन्थ होते हुए भी मौर्य पूर्व तथा मौर्यकालीन
राजनीतिक अवस्था पर प्रकाश डालता है। इसी तरह पातंजलि का ‘महाभाष्य’ भी राजनीति के संबंध में चर्चा करता है। ‘शुक्रनीतिसार’ भी एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रन्थ है जिसमें तत्कालीन
भारतीय समाज का वर्णन मिलता है। ज्योतिष ग्रन्थ गार्गी संहिता पुराण का एक भाग है
जिसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। कालिदास का ‘मालविकाग्निमित्र’ साहित्यिक होते हुए भी ऐतिहासिक सामग्रियाँ प्रस्तुत करता
है। इस ग्रन्थ में कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा विदर्भराज
की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा का उल्लेख किया है।
(ख) विदेशी विवरण–देशी लेखकों के अतिरिक्त विदेशी लेखकों के साहित्य से भी
प्राचीन भारत के इतिहास पृष्ठ निर्मित किये गये हैं। अनेक विदेशी यात्रियों एवं
लेखकों ने स्वयं भारत की यात्रा करके या लोगों से सुनकर भारतीय संस्कृति में
ग्रन्थों का प्रणयन किया है। इनमें यूनान, रोम, चीन,
तिब्बत, अरब आदि देशों के यात्री शामिल हैं। यूनानियों के विवरण
सिकन्दर के पूर्व, उसके समकालीन तथा उसके पश्चात की परिस्थितियों से संबंधित हैं। स्काइलेक्स
पहला यूनानी सैनिक था जिसने सिन्धु नदी का पता लगाने के लिए अपने स्वामी डेरियस
प्रथम के आदेश से सर्वप्रथम भारत की भूमि पर कदम रखा था। इसके विवरण से पता चलता
है कि भारतीय समाज में उच्चकुलीन जनों का
काफी सम्मान था। हेकेटियस दूसरा यूनानी लेखक था जिसने भारत और विदेशों के बीच कायम
हुए राजनीतिक संबंधों की चर्चा की है। हेरोडोटस जो एक प्रसिद्ध यूनानी लेखक था, ने यह लिखा है कि भारतीय युद्ध प्रेमी थे। इसी लेखक के
ग्रन्थ से यह भी पता चलता है कि भारत का उत्तरी तथा पश्चिमी देशों से मधुर संबंध
था। टेसियस ईरानी सम्राट जेरेक्सस का वैद्य था जिसने सिकन्दर के पूर्व के भारतीय
समाज के संगठन रीति रिवाज, रहन-सहन इत्यादि का वर्णन किया है। पर इसके विवरण अधिकांशतः कल्पना प्रधान और
असत्य हैं।
सिकन्दर के समय में भी ऐसे अनेक लेखक थे जिन्होंने भारत के
संबंध में ग्रन्थों की रचना की। ये लेखक सिकन्दर के भारत पर आक्रमण के समय ही उसके
साथ भारतवर्ष आये थे। इनमें अरिस्टोबुलस, निआर्कस, चारस, यूमेनीस आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सिकन्दर के पश्चात्
कालीन यात्रियों और लेखकों में मेगास्थनीज, प्लनी, तालिमी, डायमेकस, डायोडोरस, प्लूटार्क, एरियन, कर्टियस, जस्टिन, स्ट्रेबो आदि के नाम उल्लेख मेगास्थनीज यूनानी शासक
सेल्यूकस की ओर से राजदूत के रूप में चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी
‘इण्डिका’ भारतीय संस्थाओं भूगोल समाज के वर्गीकरण, पाटलिपुत्र आदि के संबध में प्रचुर सामग्रियाँ देती हैं।
यद्यपि इस ग्रन्थ का मूल रूप अप्राप्य है, पर इसके उद्धरण अनेक लेखकों के ग्रन्थों में आये हैं।
डायमेकस राजदूत के रूप में बिन्दुसार के दरबार में कुछ दिनों तक रहा जिसने अपने
समय की सभ्यता तथा राजनीति का उल्लेख किया है। इस लेखक की भी मूल पुस्तक अनुपल्बध
है तामली ने भारतीय भूगोल की रचना की। प्लिनी ने अपने ‘प्राकृतिक इतिहास’ में भारतीय पशुओं, पौधों, खनिज आदि का वर्णन किया। इसी प्रकार एरेलियन के लेख तथा कर्टियस, जस्टिन और स्ट्रेबो के विवरण भी प्राचीन भारत इतिहास के
अध्ययन की सामग्रियाँ प्रदान करते हैं। ‘इरिथियन’ सागर का पेरिप्लस’ नाम ग्रंथ जिसके रचयिता का नाम अज्ञात है, भारत के वाणिज्य के संबंध में ज्ञान देता है।
टैग: अथर्ववेद, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, आवश्यक सूत्र, इरिथियन सागर का पेरिप्लस, उत्तराध्ययन सूत्र, उपनिषद, ऋग्वेद, एरियन, ऐतरेय, कथा-कोष, कर्टियस, कल्प सूत्र, कल्हण, कालिका पुराण, कालिदास, कौटिल्य, गार्गी संहिता, छान्दोन्य, जस्टिन, डायमेकस, डायोडोरस, तालिमी, तैतरीय, त्रिपिटक, त्रिलोक प्रज्ञस्ति, दिव्यावदान, दीपवंश, पंचविश, पतंजलि, पराशर स्मृति, परिशिष्टपर्वन, पाणिनी, पातंजलि, पुण्याश्रव-कथाकोष, पुराण, पेरिप्लस आफ़ द इरिथियन सी, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास साहित्यिक साधन, प्राचीन-भारत, प्लनी, प्लूटार्क, बृहदारण्यक, ब्रह्माण्ड, ब्राह्मण, भद्रबाहु चरित्र, भविष्य, भागवत पुराण, मत्स्य, मनु, महाबोधिवंश, महाभारत, महाभाष्य, महावंश, महावस्तु, मालविकाग्निमित्रम, मिलन्दिपन्हो, मेगास्थनीज, यजुर्वेद, याज्ञवल्क्य नारद, राजतरंगिणी, रामायण, वायु, विष्णु, वृहस्पति, वेद, वेदांग, वैदिक मन्त्र, शतपथ, संहिता, सामवेद, स्ट्रेबो, स्मृति, स्मृतियाँ, हेरोडोटस
भारतीय इतिहास के प्राचीनतम वैभव की परिकल्पना को तब जोरदार बल मिला जब १९२१
मे दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई।
2500 ई. पू.. के लगभग भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से एक ऐसी
विकसित सभ्यता का ज्ञान 1921 ई. में लोगों के समक्ष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो केन्द्रों की खुदाई से
आना आरम्भ हुआ जिसकी तुलना में तत्कालीन विश्व की प्राचीनतम अन्य सभ्यताएं अपने
विकास के क्रम में बहुत पीछे छूट जाती है। इस सभ्यता के ज्ञान से भारतीय इतिहास का
आद्यैतिहासिक काल बहुत पहले चला जाता है। यह इस देश का गौरव रहा है कि पश्चिमी
विश्व जब जंगली सभ्यता के आंचल में ढँका था तो एशिया महाद्वीप के इस भारत देश में
एक अत्यन्त विकासमान सभ्य लोग रहते थे। इनका ज्ञान पुस्तकों से नहीं, उनकी लिखित सामाग्रियों से नहीं और न उनके पठनीय लेखों से
अपितु वहां कि उत्खनित सामाग्रियों से प्राप्त होता है। उनकी सभ्यता में धर्म का
पक्ष अत्यन्त समुन्नत था। एशिया की समकालिक अन्य पुरातन सभ्यताओं मिश्र, बाबुलोनियाँ आदि में धर्म का वह बहुविधीय स्वरूप हमें नहीं मिलता
न इतना वैज्ञानिक पैठ ही मिलता है जितना हड़प्पा की सभ्यता में।
इस सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में होने के कारण इसे
सिंधु सभ्यता तथा इसके प्रथम उत्खनित एवं विकसित केन्द्र हड़प्पा के नाम पर
हड़प्पा सभ्यता एवं आद्यैतिहासिक कालीन होने के कारण आद्यैतिहासिक भारतीय सभ्यता
आदि नामों से जानते हैं। इनका विस्तार
बलुचिस्तान, सिन्ध, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तरप्रदेश आदि विस्तृत क्षेत्र में था। ऐसा
उत्खनन से ज्ञात होता है। इन सभी क्षेत्रों में स्थिति केन्द्रों की खुदाई से समान
सभ्यता के अवशेष मिलते है। अतः इस व्यापक भाग में उस समय हड़प्पा धर्म अवश्य ही
पल्लवित रहा होगा।
हड़प्पा धर्म के स्वरूपों के विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार उसकी प्रमुख
विशेषताएं निम्न ज्ञात होती हैं-
1. इस
सभ्यता में प्रकृति से चलकर देवत्व तक की यात्रा धर्म ने तय की थी। एक ओर हम वृक्ष
पूजा देखते हैं तो दूसरी ओर पशुपति शिव की मूर्ति तथा व्यापक देवी पूजा।
2. यहाँ
देवता और दानव दोनों ही उपास्य थे। देव मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक दानवीयस्वरूपों
का यहाँ के ठीकड़ों या मुहरों पर आरेखन इस बात का परिचायक है। वृक्ष से लड़ता शेर
दानवीय भावना का उदगार ही तो कहा जा सकता है।
3. धर्म
में आध्यात्म और कर्मकाण्ड दोनों ही यहां साथ उभरे हैं। यहाँ से प्राप्त धड़ विहीन
ध्यानावसित संन्यासी की आकृति एक ओर आध्यात्मिक चेतना को उजागर करती है तो दूसरी
ओर देवी के सम्मुख पशुबलि के लिए बँधे बकरे की आकृति जो ठिकड़े पर अंकित है
कर्मकाण्ड की गहनतम भावना का घोतक है।
4. उपासना
इसका एक व्यापक अंग रहा है। नृत्य संगीत आदि के बीच देवी की पूजा को प्रदर्शित
करने वाला ठिकड़ा भी यही व्यक्त करता है।
5. कुछ
ऐसे धर्मों की जानकारी यहाँ के ठिकड़ो से मिलती हैं जिसकी सूचना इस सभ्यता के पतन
के लगभग एक हजार वर्ष बाद हमें लिखित
साहित्य प्रदान करते हैं जैसे मातृ देवियों की उपासना।
6. प्रतीकों
को धर्म में स्थान प्राप्त हो चुका था। सूर्य की तरह गोल रेखा वाली उभरती आकृति, स्वस्तिक आदि इस तथ्य के पोषक हैं कि भले ही विष्णु की
मूर्ति यहाँ नहीं मिली पर वैष्णव धर्म के प्रतीक यहाँ विद्यमान थे।
7. धार्मिक
मान्यता और विश्वासों का यह युग था। यहाँ शिवलिंग के नीचे गड़े ताबीजों की तरह के
पत्थर के टुकड़े मिले हैं। जिसके एक किनारे पर छिद्र बने हैं। सम्भवतः शिव के
द्वारा अभिमंत्रित करने के लिए ही ये लिंग के के नीचे गाडे़ गये होंगे। अन्य कुछ
ठिक़डो में मानव देवताओं के साथ नृत्य संगीत तथा धार्मिक उत्सवों को मना रहे हैं।
8. मंत्र-तंत्र
में भी इनका विश्वास रहा होगा। मुहरों पर
बने चिन्हों के ऊपर कुछ अपठनीय लिपि में लिखा है। इसे कोई चित्रांकित लिपि कहता है, कोई मात्र रेखा समूह मानता है। पर ये मंत्र रहे होगें। कुछ
मुहरों पर तो विचित्र रेखाएं बनाई गई हैं मानो आज के जंत्र-तंत्र हो।
9. लोक-धर्म
का भी यहां चलन था। कुछ मुहरों पर घेरों के भीतर वृक्ष में कुछ में फण निकाले नाग
की आकृति आदि लोकजीवन की धार्मिक भावना को व्यक्त करते हैं।
Ø प्रमुख धार्मिक स्वरूप
(1) शैव धर्म
(i) पशुपति मूर्ति :- यहाँ एक मुहर मिली है। इस पर एक तिपाई पर
एक व्यक्ति विराजमान है। इसका एक पैर मुड़ा है और एक नीचे की ओर लटका है। इसके तीन
सिर हैं तथा सिर पर तिन सींग हैं। इसके हाथ दोनों घुटनो पर हैं तथा इसकी आकृति
ध्यानावस्थित है। इसके दोनों ओर पशु हैं। इसकी छाती पर त्रिशूल की आकृति अंकित
हैं। मार्शल के अनुसार सिंधुघाटी से मिली
यह मूर्ति आज के शंकर भगवान की है। मैके ने भी इसे शिव की मूर्ति माना है। कुछ लोग
इसे पशुपति की मूर्ति मानते हैं। जो भी हो या शिव के पशुपति रूप की मूर्ति
निर्विवाद लगती है। इसके तीन सिर शिव के त्रिनेत्र के द्योतक हैं तथा तीन सींघ शिव
के त्रिसूल के प्रतीक स्वरूप है।
(ii) नर्तक शिव :- यहाँ से प्राप्त दो कबन्ध प्रस्तर मूर्तियाँ
जो पैरों की भावभंगिमा के कारण नृत्य की स्थिति का बोध कराती हैं नर्तक शिव की
मानी जाती हैं। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें नृत्यमुद्रा में उर्ध्वलिंगी होने का भी
अनुमान लगाया है।
(iii) योगी शिव :- यहाँ के एक मुहर पर योग मुद्रा में ध्यान की
स्थिति बैठे शिव की आकृति का अंकन है। इसके सामने दो तथा दोनों बगल में बैठी एक-एक
सर्प की आकृति बनी है।
(iv) बनचारी शिव :- शिव का एक रूप बनवासी का भी होता है। यहाँ एक
मुहर पर तीर-धनुष चलाते हुए एक आकृति मिली है। इसे शिव का बनचारी रूप माना जाता
है।
(v) लिंग पूजा :- बड़े तथा छोटे शिव लिंग यहाँ बहुत से मिले
हैं। कुछ के ऊपर छेद हैं जैसे ये धागा में पिरोकर गले में पहनने के काम आते होंगे।
बड़े लिंग चूना पत्थर और छोटे घोंघे के बने हैं। इनकी पूजा विभिन्न समुदायों
द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से करने का अनुमान लगाया जा सकता है।
इन विविध प्रकार की शिव मूर्तियों की प्राप्ति के आधर पर अनुमान किया जा सकता
है कि
(अ) शिव आर्यों के पूर्व भारत के मूल निवासियों, जंगली कबीलों तथा आर्येतर जातियों के देवता प्रारम्भ से रहे
हैं। इसी से इनका रंग काला था जबकि आर्य
गौर वर्ण के थे। अगर यह आर्यों के देवता रहे होते तो इनका भी रंग गोरा ही वर्णित
होता। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि जंगली पशु उनके साथ जुड़े हैं जैसे
सर्प,
सांढ़ आदि। जंगली कबीलों के लोग शक्तिशाली होते हैं तभी शिव
शक्ति के देवता के रूप में भी भारतीय जीवन में घुल-मिले हैं। इनके साथ लगा होता है
वाहन नन्दी, बैल जो
शक्ति का प्रतीक है। सांप भी इसी प्रकार का एक जुझारू जीव इनके साथ जुड़ा है। ये
बलशाली और वन्य पशु हैं जो शिव के साथ जुड़े होते हैं।
(ब) शिव को उत्पादन के देवता के रूप में भी पूजा जाता था।
शिव के साथ सांढ़ का साहचर्य उनके उस काल के उत्पादक देवता होने का बोधक है । आज
भी कृषि में उत्पादन के लिए सांढ़ों तथा बैलों का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का
यहाँ मिलना डॉ.डी.डी. कौशम्बी के अनुसार, उत्पादन का द्योतक है।
(स) प्राचीन भारत में शिवपूजा का श्रीगणेश हड़प्पा निवासियों
के समय से ही माना जाता सकता है। शिव के विविध रूप मानवाकृति, लिंगायत, पशुपति आदि इसी समय से प्रचलन में आ चुके थे। यही पीछे चलकर
हिन्दू शैव परिवार में अलग-अलग धार्मिक सम्प्रदायों के रूप में प्रमुख स्थान ग्रहण
कर लिए।
(द) योग मुद्रा की शिव मूर्तियों से स्पष्ट है कि योग क्रिया
का विकास भी शिव के साथ जुड़ा है। यह मान्यता है कि उनकी योगसाधना अनादिकाल से चली
आ रही है। योग कि विधि का भी बहुत कुछ ज्ञान यहां से उनकी प्राप्त विभिन्न योग
मुद्राओं की मूर्तियों से परिलक्षित होता है। यहाँ से आगे चलकर पशुपति योग का
विकास हुआ। यहाँ से प्राप्त संन्यासी की धड़ मूर्ति जिसकी आंखें अर्ध निमीलित हैं, ध्यान केन्द्रित है तथा उसकी आंखे नासिकाग्र पर टिकी हैं
आदि विशेषताएं ही योग साधना का पहला आधार बना होगा। यही योग का पहला चरण है। अतः
योग का प्रारम्भ भी शैव धर्म का देन रहा होगा।
(य) शंकर का नाम पौराणिक काल में भूतनाथ प्रसिद्ध हुआ। पर
भूत-प्रेतों के प्रति लोगों का विश्वास सिंधु सभ्यता के समय से ही उभर चुका था और
सम्भव है कि उस समय शंकर ही उनके स्वामी रहे हों। तब भी शुभ-अशुभ प्रभावों की
मान्यताएं थीं। इनसे बचने के लिए योनिपूजा भी सिन्धु सभ्यता में प्रचिलित थी। कुछ
विशिष्ट बीमारियों का संकेत यहां से उपचारात्मक सामग्रियों के प्राप्ति से होती है
जैसे बारहसिंगे की सींग का भस्म आदि इनसे छुटकारा पाने के लिए ही छोटे-छोटे लिंगों
को योनि के साथ ताबीज की तरह गले में धारण करते होंगे। इसी से सिंधु घाटी में बहुत
से ऐसे योनि युक्त शिवलिंग के तरह की कोणाकार पत्थर का आकृतियां मिली हैं जिनके
ऊपरी भाग में सम्भवतः धागा पिरोने के लिए छिद्र बने हैं। इससे यह भी अनुमान लगाया
जा सकता है कि बीमारियों का सम्बन्ध भी तब शिव से माना जाता होगा तथा उनके उपचार
के लिए शिवलिंग का धारण करना टोटका के रूप में मानते होंगे।
(2) वैष्णव धर्म
स्पष्ट से तो नहीं कहा जा सकता है कि हड़प्पावासी वैष्णव धर्म को मानते थे
क्योंकि विष्णु या उनके अवतारों की मूर्तियां यहां नहीं मिली हैं। पर वहाँ से
प्राप्त कुछ मुहरों पर बनी स्वस्तिक की आकृति तथा सूर्य का चिन्ह इस बात का द्योतक
है कि पीछे वैष्णव सम्प्रदाय के विकास के साथ जुड़ने वाले ये प्रतीक बीज रूप में
जुड़े थे। अतः वैष्णव सम्प्रदाय वहां अस्तित्व में भले ही विकसित रूप में न आया हो
पर इसका बीजारोपण इस समय हो चुका था इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
(2) शाक्य सम्प्रदाय
शक्ति पूजा प्राची विश्व की प्रायः सभी सभ्यताओं में होती रही है तभी शक्ति को
आदिशक्ति माना जाता है। सिंधुघाटी से भी देवी की उपासना के चिन्ह प्राप्त होते
हैं। सिन्धु सभ्यता में एक मुहर पर अंकित एक स्त्री की नाभि से निकला हुआ कमलनाल
दिखाया गया है। यह उत्पादन एवं उर्वरता का बोधक होता है। शक्ति की उपासना पृथ्वी
पूजा से जुड़ी है। वहीं से मातृदेवी की उपासना का प्रारम्भ माना जाता है। यहाँ इन
सभी का सम्बन्ध पृथ्वी देवी से और पौधों का सम्बन्ध उर्वरता तथा सृजनशीलता से
जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें देवी पालथी मारे
बैठी है और उनके दोनों ओर पुजारी भी बैठे
हैं तथा इसके सिर पर एक पीपल का वृक्ष उगा
है। इसको भी उत्पादकता का ही प्रतीक माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या
में मातृदेवियों की मूर्तियों का यहां मिलना द्योतक है कि ये लोग देवी के उपासक थे
इनकी देवियाँ अविवाहित कन्याएँ होती थीं क्योंकि उनके स्तन सामान्य उभार के तथा
गोल और अविकसित दीखते हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों तथा केशविन्यास से सज्जित
देवियों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विविध देवियों की मान्यता यहाँ
रही होगी अन्यथा सर्वत्र एक ही प्रकार की देवी मूर्तियाँ प्राप्त होतीं। एक बात और
ज्ञात होती है कि ये प्रकृति को मातृदेवी के रूप में मानते थे तभी देवियों के साथ
प्रकृति अवयव यहाँ जुड़ा मिला है। प्रकृति के ही सहारे जीव का पोषण होता है
सम्भवतः ऐसा इनका विश्वास था।
एक मुहर पर सात औरतों की खड़ी आकृतियाँ बनी हैं और उनके सामने एक बकरा बँधा है जिसके
पीछे लोग ढोल बजाते हुए नाच रहे हैं। देवी उपासना की पौराणिक परम्परा में
सप्तमातृका एवं नवमातृका के उपासना का वर्णन मिलता है। यहाँ भी सप्तमातृका के
उपासना का बोध होता है इस मुहर पर सात औरतों का अंकन इसका बोधक है। दूसरी ओर
पौराणिक शाक्तधर्म में देवी के लिए पशुबली की मान्यता समाज में प्रचिलित है। यहाँ एक मुहर पर बँधा बकरा
बलि के लिए उपस्थिति प्रतीत होता है। पौराणिक देवी पूजन का आरम्भ इसे मान सकते
हैं। यहाँ से प्राप्त नारी मूर्तियों में एक विशेषता मुख्य रूप से दीखती है कि वे निर्वस्त्र हैं। निर्वस्त्रता प्रकृति के
खुलेपन तथा उत्पादन का बोधक है। इससे हम कह सकते हैं कि ये प्रकृति को मातृदेवी
मानकर उपासना करते थे इनकी पुष्टि यहां के एक मुहर पर प्राप्त एक देवी की मूर्ति
से होती है जिसके सिर पर चील की तरह एक पक्षी पंख फैलाए बैठा है। लगता है कि वह
मातृदेवी की रक्षा कर रहा हो।
(3) वृक्ष-पूजा
पौराणिक काल से पीपल, नीम,
आंवला आदि वृक्षों की पूजा समाज में की जाती है तथा इससे
सम्बन्धित अनेक त्योहारों की मान्यता भी दी गई है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी
वृक्ष पूजा का चलन था तभी वहाँ से प्राप्त ठीकरों पर अनेक वृक्षों की आकृतियाँ
अंकित हैं। इनसे पत्तों के आधार पर पीपल के वृक्ष की पहचान तो हो जाती है पर यह
असंभव नहीं कि इसी प्रकार अन्य वृक्षों की भी महत्ता इस समय रही हो। एक ठिकड़े पर
बनी आकृति में एक सींगवाले पशु के दो सिर बने हैं जिनके ऊपर पीपल की कोमल पत्तियाँ
फूटती हुई दीखती हैं। दीर्घायु, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के कारण आज की तरह उस, समय भी संभवतः पूज्य मान लिया गया होगा। सम्भवतः तब से अब
तक उसकी धार्मिक महत्ता बनी रही।
ऋग्वेद
में अश्वत्थ की महत्ता का उल्लेख भी पीपल का ही बोधक है। दूसरी मुहर पर देवता की
नग्न मूर्ति बनी है। उनके दोनों ओर पीपल की दो शाखाएं अंकित हैं। यहां की एक मुहर
वन्दना की मुद्रा में झुकी एक मूर्ति है जिसके बाल लम्बे हैं। उसके पीछे मानव के
चेहरे वाले वृष तथा बकरे की मिली जुली आकृति अंकित है। सामने पीपल का पेड़ है लगता
है कि ये पशु वृक्ष देवता के वाहन के रूप में अंकित किए गए हैं। शुंगकला में सांची
तथा भरहुत में ऐसे वृक्ष देवियों की अनेक आकृतियाँ अंकित हैं जिन्हें दोहद की
अवस्था में अंकित यक्षिणी कहा जाता है। इन भिन्नताओं के आधार पर डॉ. मुखर्जी के अनुसार
वहां पर दो प्रकार की वृक्ष-पूजा प्रचलित थी-एक वृक्ष की पूजा तथा दूसरे वृक्ष
अधिदेवता की पूजा।
(4) पशु-पूजा
वहां कि मुहरों पर अनेक प्रकार के पशुओं का अंकन मिला है। विविधता और संख्या
में पशु अंकन की अधिकता को देखकर ऐसा लगता है कि ये पशुओं को देवता का अंश मानते
थे। यह विश्वास है कि पहले पशुओं के रूप में देवताओं को स्वीकार किया जाता था।
पीछे इनका मावनवीय रूप अंगीकार किया गया। इसीसे देवता प्रत्येक पुरातन सभ्यता में
पशु-पूजा का चलन मिलता है। इसका प्रमाण है कि प्रायः प्रत्येक देवता के साथ एक
वाहन का जुड़ा होना आज भी स्वीकार किया जाता है। दूसरे इस सभ्यता में हम देखते हैं
मनुष्यों के रूप में निर्मित देवताओं के सिर पर सींग धारण करने की कल्पना यहां
किया गया था। सींग को शक्ति का प्रतीक माना जाता था इसीसे इसको मानव रूप धारी देव
भी कहते थे। इसीलिए आज जिन्हें हम देवतावाहन मानते हैं जैसे-गैंडा, बैल, हाथी,
भैंस, कुत्ता आदि इनके भी चित्रण यहां की मुहरों पर मिलते हैं।
बैल की पूजा विशेष रूप से यहां होती होगी क्योंकि इसके
विविध प्रकारों का अंकन यहां के मुहरों पर बहुतायाद से दीखता है जैसे एक श्रृंगी, कूबड़दार, लम्बी लटकी लोरदार आदि। लगता है शिव के साथ बैल का सम्बन्ध
इसी सभ्यता से शुरू हुआ था क्योंकि यहां इन दोनों की साथ आकृतियाँ मुहरों पर
बहुलता से अंकित मिलती हैं। कुछ पशु ऐसे भी बने हैं जो काल्पनिक प्रतीत होते हैं।
आज भी उनका वास्तविक शिवरूप प्राप्त नहीं होता। इनमें हम ऐसे पशुओं को ले सकते हैं
जिनकी रचना विभिन्न पशुओं के अंगों के योग से की गई हैं। अन्यथा ये मानव और पशु की
मिली जुली मूर्ति हों। एक ठिकड़े पर मानव सिर से युक्त बकरे की आकृति है। एक पर
ऐसा पशु है जिसका सिर गैंडे का पीठ किसी दूसरी पशु की पूंछ किसी अन्य पशु की है।
कुछ पशुओं की ऐसी आकृतिया यहां बनी हैं जिनके सामने नाद बना है और वे उसमें से कुछ
खाते हुए दीखते हैं। कितने पशुओं की खोपड़ी धूपदानी की तरह कटोरानुमा बनी है।
इनमें सम्भवतः पूजा के समय धूप जलाया जाता होगा क्योंकि उनके किनारों पर धुंए के
चिन्ह पड़े हैं। लगता है कि पशु-पूजन में धूप जलाने का भी प्रचलन था।
(5) जैन धर्म
सिंधु घाटी की मूर्तियों में बैल की आकृतियाँ विशेष रूप से मिलती हैं। ‘वृषभ’ का अर्थ है बैल। आदिनाथ या वृषभनाथ जो जैन धर्म के प्रवर्तक
थे उनका चिन्ह बैल है। सिंधु घाटी से प्राप्त बैल की आकृति सूचक है कि उस समय
जैनधर्म का बीजारोपण हो चुका होगा। यहां से प्राप्त एक नंगी कबन्ध मूर्ति जो
ग्रेनाइट पत्थर की बनी है उसे कुछ विद्वान जैन धर्म से सम्बन्धित मूर्ति मानते हैं
क्योंकि जैनियों कि नग्न मूर्तियों की तरह यह है। दिगम्बर समुदाय वाले जैन भिक्षु
नग्न ही रहते हैं। तीसरे यहां की एक मूर्ति को मार्शल ने कार्योत्सर्ग नामक योगासन
में खड़ा बतलाया है। इससे लगता है कि योग की क्रिया जो जैनियों में व्यापक थी यहीं
से प्रारम्भ हुई। इसलिए भी यह माना जा सकता है कि उक्त मूर्ति का सम्बन्ध जैन धर्म
से रहा होगा।
Ø मान्यता और विश्वास
(अ)-स्वच्छता- इसके ये पुजारी थे। इसी से यहां विशाल
स्नानागार तथा गर्म स्नानागार बने हैं। ये सामूहिक स्नान के लिए बनाए गए।
व्यक्तिगत स्नान के लिए प्रत्येक घर के आंगन में स्नानगृह होता था। लगता है
उत्सवों तथा पर्वों पर आज के पौराणिक धर्म की मान्यता की तरह लोग सामूहिक स्नान
करते होंगे। तभी विशाल स्नान घर की आवश्यता पड़ी होगी।
(ब) मृतक संस्कार- मृतक क्रिया में इनका विश्वास था। मरने के
बाद ये शरीर की क्रिया करते थे। उसे गाड़ते या जलाते थ। जलाने के बाद बची हुई
हड्डियों को एकत्रित करके किसी बर्तन में रखकर उसे प्रवाहित कर देते थे। कभी-कभी
तो इसे गाड़ भी देते थे। जिन मृतकों को गाड़ते थे उनके साथ उनकी प्रिय वस्तुएं भी
गाड़ दी जाती थीं। यही प्रथा प्राचीन मिश्र के पिरामिडों में भी दीखती है। इसका
प्रमाण है कि हड़प्पा और बलुचिस्तान में सर्वांगीण शव-निखात प्राप्त हुए हैं।
(स) जादू-टोना- यहां से प्राप्त टिकटों पर कुछ लिखा हुआ है।
लगता है ये जादुई मंत्र होंगे। इनके द्वारा लोग अपने कार्यों को सिद्ध करते होंगे।
इसी प्रकार लिंगों के नीचे गड़े ताबीज जिन पर कुछ अंकित है जादू की क्रिया का होना
सिद्ध करते हैं। सम्भव है ये ताबीजों को इसलिए पहनते होंगे कि भवबाधा इन्हें न
सतावे। इसी प्रकार कुछ ऐसे ठिकड़े भी मिले हैं जिन पर विचित्र प्रकार के चिन्ह बने
हैं। ये तांत्रिक चिन्हों की तरह हैं जिस प्रकार का प्रयोग आज तंत्र में होता है।
लगता है कि इनको विश्वास था कि इनके द्वारा बाधाओं के निराकरण में सहायता मिलती
है।
(द) बलि प्रथा- देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का
प्रयोग किया जाता था। इसके संदर्भ में जैसा हमने ऊपर देखा है कि सप्तमातृकाओं के
सामने एक बकरा बंधा है, यह बलि पशु ही रहा होगा।
(ग) धार्मिक पर्व और उत्सव – यहां कुछ मुहरों पर नृत्य,. संगीत के सामूहिक अवस्था का अंकन हुआ है। लगता है किसी
विशेष उत्सव या पर्व पर इस प्रकार के सामूहिक आमोद-प्रमोद की अवस्था का चलन था।
सामूहिक स्नान के लिए जलकुण्डों का होना सिद्घ करता है कि उस समय पर्व मनाए जाते
थे जहां लोग एक साथ एकत्रित होकर आज की पौराणिक मान्यता की तरह सामाजिक रूप से
स्नान आदि धार्मिक क्रियाएं करते होंगे।
टैग: जादू टोना, दयाराम साहनी, पशुपति की मूर्ति, मुहर,
मोहनजोदड़ो, योग मुद्रा की शिव की मूर्ति, योगी शिव, योनी, राखालदास बैनर्जी, लिंग पूजा, शिव उपसना, सिंधु घाटी सभ्यता, स्वस्तिक, हड़प्पा
लगभग 600 ई-पू-
से 600 ईसवी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक
परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा।
उदाहरणत: वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ जिससे वहा रहने वाले लोगों की
जीवनशैली में परिवर्तन हुआ शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय
हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया।
इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय: साहित्यिक परंपराओं का उपयोग
करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे। अन्य ग्रंथ समाज का
चित्रण करते थे और कभी-कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी
प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती
है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ ;और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था।
अत: यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और किनके लिए इनकी रचना हुई। इस बात पर भी
ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका
प्रचार-प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज
में प्रचलित आचार-व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है।
§ महाभारत का
समालोचनात्मक सस्कंरण
1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी-एस- सुकथांकर के नेतृत्व
में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर
महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या-क्या
कार्य थे?
आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी
गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने
वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का
एक तरीका ढूढ़ निकाला। अंतत: उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों
में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना
को पूरा करने में सैंतालीस वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से
उभर कर आइ : पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट
होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तिर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में
केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात जो
स्पष्ट हुई, वह यह
थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद
भी उभर कर सामने आए।
इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पादटिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में
किया गया। 13000
पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्योरा देते हैं। एक तरह से देखा
जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं
और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप
दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी
प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यत: उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत
में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में
इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन
ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा
गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में
विद्वानों ने पालि, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन
अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधकारिक माने जाते
थे,
किन्तु इन आदशो को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और
यदा-कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों
के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा।
2 अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता
21 परिवारों के बारे में जानकारी
हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। किन्तु आपने देखा
होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते : पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी
भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में
मिल-बाटकर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही
संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते
हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधयों को जाति समूह कह सकते हैं।
पारिवारिक रिश्ते ‘नैसर्र्गिक’ और रक्त संब, माने जाते हैं किन्तु इन संबंधों की परिभाषा अलग-अलग तरीके
से की जाती है।
कुछ समाजों में भाई-बहन ;चचेरे, मौसेरे
आदि से खून का रिश्ता माना जाता है किन्तु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। आरंभिक
समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी
से मिल जाती है किन्तु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्र्मित करना
मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण
करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता
है। संभवत: इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह
व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा।
22 पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श
क्या हम उन िबदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में
परिवर्तन आया? एक
स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों कौरव और पांडव के बीच
भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से
संबंधत थे जिनका एक जनपद पर शासन था। यह
संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक
उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालाकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले
भी मौजूद थी, महाभारत
की मुख्य कथावस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की
मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर ;राजाओं के संदर्भ में सिहासन पर भी अधिकार जमा सकते थे। अधिकतर राजवंश ;लगभग छठी शताब्दी ई-पू- से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण
करते थे। हालाकि इस प्रथा में विभिन्नता थी : कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे
का उत्तराधिकारी हो जाता था तो कभी बंधु-बांधव सिहासन पर अपना अधिकार जमाते थे।
कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रिया जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थीं। पितृवंशिकता के प्रति
झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ
के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और
ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे।
23 विवाह के नियम
जहा पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे वहा इस व्यवस्था में
पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं
था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को
बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले
परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया
जाता था जिससे ‘उचित’ समय और ‘उचित’
व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि
कन्यादान अर्थात् विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य
माना गया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहा पर निकट और दूर
से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद-फ़रोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में
विचारों का भी आदान-प्रदान होता था। संभवत: इस वजह से आरंभिक विश्वासों और
व्यवहारों पर प्रश्नचिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के
लिए विस्तृत आचार संहिताए तैयार कीं।
ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था किन्तु बाकी समाज
को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ई-पू- से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र
नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी जिसका
संकलन लगभग 200 ई-पू-
से 200 ईसवी के बीच हुआ। हालाकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का
यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा
पालन होना चाहिए, किन्तु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में
रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की
वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि
धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के आठ प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें
से पहले चार ‘उत्तम’ माने जाते थे और बाकियों को निदित माना गया। संभव है कि ये
विवाह पद्धतिया उन लोगों में प्रचलित थीं जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते
थे।
24 स्त्री का गोत्र
एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ई-पू- के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों ;खासतौर से ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक
वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों
के दो नियम महत्वपूर्ण थे : विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के
गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते
थे। क्या इन नियमों का सामान्यत: अनुसरण होता था, इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का
विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी-कभी गोत्रों के नाम से उ,द्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों
के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था
;लगभग दूसरी शताब्दी ई-पू से दूसरी शताब्दी ईसवी तक। सातवाहनों
के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक
रिश्तों का खाका तैयार किया है। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा ;अर्थात् एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन
राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता
है कि उनके नाम गौतम तथा वसिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे जो उनके पिता के गोत्र थे।
इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की
अपेक्षा,
जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा।
यह भी पता चलता है कि कुछ रानिया एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य बहिर्र्विवाह
पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुत: यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह
पद्धति अर्थात् बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है जिसका प्रचलन दक्षिण भारत
के कई समुदायों में अभी भी है। बांधवों ;ममेर, चचेरे इत्यादि भाई-बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह
से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवत: उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य
विविधताए भी मौजूद थीं किन्तु उनके विशिष्ट ब्योरों को पुननिर्मित करना संभव नहीं
हो पाया है।
25 क्या माताए महत्वपूर्ण थीं?
हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम ;माता के नाम से उद्भूत से चित्रित किया जाता था। इससे यह
प्रतीत होता है कि माताए महत्वपूर्ण थीं किन्तु किसी भी निष्कर्ष पर पहुचने से
पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात
है कि सिहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था।
3 सामाजिक विषमताए
वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे संभवत: आप ‘जाति’ शब्द से परिचित होंगे जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को
दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया
गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा
प्राप्त है, एक
दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और ‘अस्पृश्यों’ को
सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवत: जन्म के अनुसार
निधार्रित माना जाता था।
31 ‘उचित’ जीविका
धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वगो के लिए आदर्श ‘जीविका’ से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था तथा उनका काम दान देना और लेना था।
क्षत्रियों का कर्म यद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान-दक्षिणा देना था। अंतिम तीन कार्य
वैश्यों के लिए भी थे साथ ही उनसे कृषि, गौ-पालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए
मात्र एक ही जीविका थी तीनों ‘उच्च’
वर्णों की सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए
ब्राह्मणों ने दो-तीन नीतिया अपनाइ। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय
व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों
में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म
पर आधारित है। किन्तु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अत: इन मानदंडों को बहुधा
महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वणित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था।
32 अक्षत्रिय राजा
शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे। किन्तु अनेक महत्वपूर्ण
राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश जिसने एक विशाल
साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित
किया गया है कि वे क्षत्रिय थे किन्तु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें ‘निम्न’ कुल का मानते हैं। शुंग और कण्व जो मौयो के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुत: राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह
व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म
लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को, जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण उन्हें मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्यदेशीय मानते थे। किन्तु संस्कृत के संभवत:
आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन ;लगभग दूसरी शताब्दी ईसवीद द्वारा सुदर्शन सरोवर के
जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है।
इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली
मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के
सबसे प्रसिद्ध शासक गोतमी-पुत्त सिरी-सातकनि ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही
क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि चार
वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई। किन्तु फ़िर भी रुद्रदामन के
परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया
थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के
अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने
का दावा करते थे किन्तु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो
इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे और जैसा हमने देखा वह अंतर्र्विवाह पद्धति का पालन
करते थे न कि बहिर्र्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है।
33 जाति और सामाजिक गतिशीलता
ये जटिलताए समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति
से भी स्पष्ट होती हैं। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर
आधारित थी। किन्तु वर्ण जहा मात्र चार थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं
थी। वस्तुत: जहा कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना-सामना हुआ – उदाहरणत: जंगल में रहने वाले निषाद या कि व्यावसायिक वर्ग
जैसे सुवर्णकार, जिन्हें
चार वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातिया जो एक ही
जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थीं उन्हें कभी-कभी श्रेणियों में भी संगठित किया
जाता था। हालाकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा-जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किन्तु कुछ अपवाद हैं जैसे कि मंदसौर ;मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख ;लगभग पाचवीं शताब्दी ईसवी। इसमें रेशम के बुनकरों की एक
श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलत: लाट ;गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहा से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा
उन्होंने अपने बच्चों और बांधवो के साथ संपन्न की। उन्होंने वहा के राजा की महानता
के बारे में सुना था अत: वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक
प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि
प्रदान करता है। हालाकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। कुछ
सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक
व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने
शिल्पकर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया।
34 चार वर्णों के परे : एकीकरण
उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहा हमेशा से ऐसे समुदाय
रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य
में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और शुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन
प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार और कंद-मूल संग्रह करना
जीवन-निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका
की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के साचे
के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा-कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था। किन्तु इन
लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान-प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के
बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है।
35 चार वर्णों के परे : अधीनता और संघर्ष
ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे।
साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वगो को ‘अस्पृश्य’ घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया।
ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खासतौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और ‘पवित्र’ थे, अत: अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों उपमहाद्वीप
के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक
ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में एक लाख
श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा-जोखा है।
इस ग्रंथ की रचना एक हजार वर्ष तक होती रही ;लगभग 500 ई-पू- से। इसमें निहित कुछ कथाए तो इस काल से पहले भी
प्रचलित थीं। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए यद्ध का चित्रण है। इस
ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार-व्यवहार के मानदंड तय करते
हैं।
यदा-कदा ;किन्तु
हमेशा नहीं इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई
पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है? भोजन
नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे
जिन्हें खासतौर से ‘दूषित’ माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने
वालों को चांडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि
में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊ…पर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श, यहा तक कि उन्हें देखना भी, अपवित्रकारी मानते थे।
मनुस्मृति में चाडालों के ‘कर्तव्यों’ की
सूची मिलती है। उन्हें गाव के बाहर रहना होता था। वे फेके हुए बर्तनों का इस्तेमाल
करते थे,
मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे।
रात्रि में वे गांव और नगरों में चल-फ़िर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों
की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधक के रूप में भी कार्य करना होता था। चीन
से आए बौद्ध भिक्षु फाह-शिएन ;लगभग पाचवीं शताब्दी ईसवी, का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर
अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाए। एक
और चीनी तीर्थयात्री श्वैन-त्सांग ;लगभग सातवीं शताब्दी ईसवी कहता है कि वधक और सफ़ाई करने
वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के
जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या
चांडालों ने शास्त्रों में निधार्रित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था? यदा-कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए
चित्रण में समानता है परंतु कभी-कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत
मिलता है।
4 जन्म के परे : संसाधन और प्रतिष्ठा
यदि आप आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान,ग्राममुखिया, शिल्पकार, वणिक
और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में
उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर
उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदभो में इस बात का परीक्षण करेंगे कि
संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे।
41 संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार
अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच
लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधष्ठिर को द्यूत
क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधष्ठिर अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा धोखा दिए जाने
के कारण इस द्यूत में स्वर्ण, हस्ति, रथ, दास,
सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फ़िर स्वयं को भी दाव पर लगा कर गवा बैठे। इसके
उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दाव पर लगाया और उसे भी हार गए।
संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं।
मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता-पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों
में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए किन्तु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का
अधिकारी था। स्त्रिया इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की माग नहीं कर सकती थीं।
किन्तु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे
स्त्रीधन ;अर्थात्
स्त्री का धनद्ध की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप
में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किन्तु
मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं
अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ्य
वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा ही है। किन्तु अधिकतर अभिलेखीय व साहित्यिक साक्ष्य इस बात की ओर
इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाए संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थीं, सामान्यत: भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में, स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों
पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई।
42 वर्ण और संपत्ति के अधिकार
ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार ;लैंगिक आधार के अतिरिक्तद्ध वर्ण था। जैसा हम जानते है कि
शूद्रों के लिए एकमात्र ‘जीविका’ ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी।
हालाकि तीन उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी।
यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय
सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक
परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित
होते हैं पुरोहित भी सामान्यत: धनी दर्शाए जाते हैं। हालाकि यदा-कदा निर्धन
ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर, जहा समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र
में संहिताबद्ध किया जा रहा था अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत
की। इनमे से सर्वविदित आलोचनाए प्रारंभिक बौद्ध धर्म में ;लगभग छठी शताब्दी ई-पू- से, विकसित
हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी किन्तु यह
भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक
प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया।
43 एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा : संपत्ति में भागीदारी
अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहा लोग अपनी संपत्ति के
आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे, या पिफर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी। किन्तु समाज
में अन्य संभावनाए भी थीं। वह स्थिति जहा दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा
कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था, घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम् एक ऐसा ही क्षेत्र
था जहा उपरोक्त आदशो को संजोया जाता था।
जैसा हम जानते है इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारिया थीं। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने
वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह
में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है जो इस ओर इंगित करता है कि
हालाकि धनी और निर्धन के बीच विषमताए थीं, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की
जाती थी कि वे मिल-बाट कर उसका उपयोग करेंगे।
5 सामाजिक विषमताओं की व्याख्या : एक सामाजिक अनुबंध
बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की।
साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की
आवश्यकता थी, उस पर
भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्तपिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह
बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित
था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण
करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती है। किन्तु यह व्यवस्था क्रमश:
पतनशील हुई।
मनुष्य अधिकाधक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि: क्या हम एक
ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे और जिसे
निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करे? बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे— सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत्त की उपाधि
प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर
निर्भर करता था। ‘कर’ वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे।
यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में
मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी हैं। उदाहरणत: यदि मनुष्य स्वयं एक
प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला
सकते थे।
इतिहासकार और महाभारत
यदि आप इस आलेख के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएगे कि इतिहासकार किसी
ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण
करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया : पालि, प्राकृत अथवा तमिल, जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी अथवा संस्कृत जो विशिष्ट
रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के
प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ ‘मंत्र’ थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चरित किए जाते थे
अथवा ये ‘कथा’ ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दुबारा
सुनाया जा सकता था? इसके अलावा इतिहासकार लेखक; के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण
और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार
परीक्षण करते हैं क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर
ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन/रचना काल और उसकी रचनाभूमि का
भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी
ग्रंथ की विषयवस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत
जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में, आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा।
भाषा एवं विषयवस्तु
अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे
हैं वह संस्कृत में है ;यद्यपि
अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं। किन्तु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत
वेदों अथवा प्रशस्तियों में वर्णित
संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अत: यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर
पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषयवस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान
तथा उपदेशात्मक-के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और
उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार-विचार के मानदंडों का चित्रण है। किन्तु यह
विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है-उपदेशात्मक अंशों में भी कहानिया होती
हैं और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस
बात पर एकमत हैं कि महाभारत वस्तुत: एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक
अंश बाद में जोड़े गए। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को ‘इतिहास’ की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है : ‘ऐसा ही था।’ क्या महाभारत में, सचमुच में हुए किसी यद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ
इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का
मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी
और साक्ष्य से नहीं होती।
लेखक-एक या कई और तिथिया
यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवत: मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे जिन्हें ‘सूत’ कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्धक्षेत्र में जाते थे और उनकी
विजय व उपलब्धियो के बारे में कविताए लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में
हुआ। पाचवीं शताब्दी ई-पू- से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया
और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल जिनके इर्द-गिर्द महाभारत की कथा
घूमती है,
मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए
राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली
उथल-पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना
हुई जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ई-पू- से 200 ईसवी के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकाल का एक और चरण देखते
हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी, तथा श्रीकृष्ण को जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में
से हैं,
उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200-400 ईसवी के बीच मनुस्मृति से मिलते-जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण
महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवधर्नों के कारण यह ग्रंथ जो अपने प्रारंभिक रूप
में संभवत: 10ए000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़ कर एक लाख श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस
बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं।
सदृशता की खोज
महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भाति युद्धों, वनों,राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बी-बी- लाल ने मेरठ जिले ;उ-प्र के हस्तिनापुर नामक एक गाव में उत्खनन किया। क्या यह
गाव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालाकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है किन्तु
गंगा के ऊ…परी
दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना जहा कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी
हस्तिनापुर हो सकता है ।
टैग: प्राचीन भारत का समाज, प्राचीन भारत की जटिल सामाजिक प्रक्रिया, प्राचीन-भारत, सामाजिक व्यवस्था
प्राचीन भारत की झलक
Posted by: संपादक- मिथिलेश वामनकर on: फ़रवरी 14, 2009
In: प्राचीन-भारत | Uncategorized 20 Comments
हड़प्पा सभ्यता के बाद डेढ़ हजार वषोरं के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के
विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिधु नदी और इसकी
उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई
क्षेत्रों में कृषक बस्तियाँ अस्तित्व में आईं। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के
क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दि
के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े-बड़े ढाँचे
मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से
बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से नए
परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक
प्रक्रयाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के
तरीके से चलता है। इसी के साथ-साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ।
इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का
अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है, और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी
कहानी नहीं मिल पाती है।
1- प्रिंसेप और पियदस्सी
भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने
ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक
अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और
सिक्कों पर पियदस्सी, यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम
अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधक प्रसिद्ध शासकों में से एक
था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नयी दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन
करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में
लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणामस्वरूप बीसवीं सदी के आरंभिक दशकों
तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद
विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने
की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और अर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच
कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे लेकिन संभवत: सीधे
संबंध हमेशा नहीं थे।
2- प्रारंभिक राज्य
2-1 सोलह महाजनपद
आरंभिक भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ई-पू- को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी
काल माना जाता है। इस काल को प्राय: आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता
है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ।
बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से सोलह राज्यों का उल्लेख
मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एकसमान नहीं है लेकिन
वज्जि,
मगध, कोशल,
कुरु, पांचाल, गांधार और अवन्ति जैसे नाम प्राय: मिलते हैं। इससे यह
स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे।
अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध
राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था, इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर
और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधत थे।
वज्जि संघ की ही भाँति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक अर्थिक स्रोतों पर राजा गण
सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी
तरह लिखे नहीं जा सकते लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग एक हजार साल तक बने रहे।
प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय: किले से घेरा जाता था।
किलेबंद राजधानियों के रख-रखाव और प्रारंभीक सेना और नौकरशाही के लिए भारी अर्थिक
स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों
ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों
का निधार्रण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे
भी देखिए। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता
था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्त जुटाने का एक वैध उपाय
पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे-धीरे कुछ
राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएँ और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी
सहायक-सेना पर निर्भर थे जिन्हें प्राय: कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था।
2 सोलह महाजनपदों में प्रथम : मगध
छठी से चौथी शताब्दी ई-पू- में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन
गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की
उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में भी
आसानी से उपलब्ध थीं जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों
में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी
उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने
मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के
अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे, और इनके मंत्री उनकी नीतियाँ लागू करते थे। प्रारंभ में, राजगृह ;आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि
इस शब्द का अर्थ है ‘राजाओं
का घर’। पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था। बाद में
चौथी शताब्दी ई-पू- में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के
मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी।
3- एक आरंभिक साम्राज्य
मगध के विकास के साथ-साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के
संस्थापक चंन्द्रगुप्त मौर्य ;लगभग 321 ई-पू-
का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक
ने जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कंलिंग आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। मौर्य साम्राज्य
के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया
है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं, विशेषतया मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुननिर्माण हेतु
समकालीन रचनाएँ भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत
मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। एक और स्रोत
जिसका उपयोग प्राय: किया जाता है, वह है अर्थशास्त्र। संभवत: इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य
या चाणक्य ने की थी जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख
परवर्ती जैन, बौद्ध
और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वांइमय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े
उपयोगी हैं लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय: सबसे मूल्यवान
स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के
लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने
अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, संन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों
और परंपराओं का आदर शामिल हैं।
3-2 साम्राज्य का प्रशासन
मौर्य साम्राज्य के पाँच प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और चार प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जयिनी, तोसलि और सुवर्णगिरि। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में
किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक
पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तरांचल तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण
किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ऐसा संभव नहीं
था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध आरै भिन्न-भिन्न प्रकार के थे : कहाँ
अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि
सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय
केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जयिनी दोनों लंबी दूरी वाले
महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे जबकि सुवर्णगिरि अर्थात् सोने के पहाड़
कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था।
साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना
अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय
लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान-पान की व्यवस्था और उनकी
सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक
प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधयों के संचालन के लिए एक समिति
और छ: उपसमितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान-पान का संचालन करती थी, तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोहियों, पाँचवीं का रथारोहियों तथा छठी का काम हाथियों का संचालन
करना था। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था : उपकरणों के ढोने के लिए
बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की
देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य को
अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा
कि हमने अभी ई…पर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के
अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में
अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्त नाम से विशेष अधिकारियों की
नियुक्ति की गई।
3-3 मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था?
उन्नीसवीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू
की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश
साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। उन्नीसवीं और आरंभिक बीसवीं सदी के भारतीय
इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण
तथा उत्साहवधर्क लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक
अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा
कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। इसमें उन्हें यह
लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ
ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी-बड़ी
उपाधयाँ जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि बीसवीं सदी के
राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना।
—————-
mauryamap
—————–
मौर्य साम्राज्य सौ साल तक ही चल पाया जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में
बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र को देखें तो पता
चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ
तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एकसमान नहीं था। दूसरी शताब्दी
ई-पू- आते-आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए-नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे।
4- राजधर्म के नवीन सिद्धात
4-1 दक्षिण के राजा और सरदार
उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात्
तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर और पाण्ड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत
ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के
स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर, प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएँ हैं जो सरदारों
का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से
किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य
और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग द्वितीय शताब्दी
ई-पू- से द्वितीय शताब्दी ई- तक और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन
करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में
अधक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में जानते है कि एक बार सत्ता में
आने के बाद उन्होंने ऊँचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया।
4-2 दैविक राजा
राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी-देवताओं के
साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण
शासकों ने ;लगभग
प्रथम शताब्दी ई-पू- से प्रथम शताब्दी ई- तक इस उपाय का सबसे अच्छा उद्धरण
प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की
गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की उसका
सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूख्रतयों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में
मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूख्रतयाँ लगाई गई
थीं। अप्फ़ागानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूख्रतयाँ मिली हैं।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूख्रतयों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य
प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे ‘देवपुत्र’ की उपाध भी लगाई थी। संभवत: वे उन चीनी शासकों से प्रेरित
हुए होंगे,जो
स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। चौथी शताब्दी ई- में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े
साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे।
अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल
था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत
शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे, वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास
साहित्य,
सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही
कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियाँ भी उपयोगी रही
हैं। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्राय:
प्रयास करते हैं लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक
ग्रंथ मानते थे। उदाहरण के तौर पर, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति
की रचना हरिषेण जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवत: सबसे शक्तिशाली सम्राट
समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कॄत में की थी।
5-1 जनता में राजा की छवि
राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं।
वस्तुत: साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम
ही छोड़े गए हैं। फ़िर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है।
उदाहरण के तौर पर, जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वख्रणत कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों
ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से-कहानियाँ हैं
जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएँ पहली सहस्राब्दि ई- के मध्य
में पालि भाषा में लिखी गईं। गंदतिन्दु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक
कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएँ, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा
अपनी पहचान बदल कर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या
सोचते हैं तो एक-एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला-बुरा कहा। उनकी शिकायत
थी कि रात में डकेत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर जमा करने वाले अधिकारी। ऐसी
परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने-अपने गाँव छोड़ कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस
कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा, के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े-बड़े कर की
माँग करते थे जिससे किसान खासतौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है
कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती
माँग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाए ढूँढ़ने शुरू किए।
5-2 उपज बढ़ाने के तरीके
उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। जो छठी शताब्दी ईपू-से ही गंगा और
कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फ़ैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी
वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फ़ाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की
जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि
होने लगी। हालाँकि किसानों को इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के
फाल वाले हल की वजह से फ़सलों की उपज बढ़ने लगी लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप
के कुछ ही हिस्से में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसी अधर्शुष्क जमीन वाले
क्षेत्रों में लोहे के फ़ाल वाले हल का प्रयोग बीसवीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान
उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे उन्होंने खेती के
लिए कुछाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं-कहीं नहरों के माध्यम से िसचाई करना था।
व्यक्तिगत लोगों और कॄषक समुदायों ने मिलकर सचाई के साधन निख्रमत किए। व्यक्तिगत
तौर पर तालाबों, कुओं
और नहरों जैसे िसचाई साधन निख्रमत करने वाले लोग प्राय: राजा या प्रभावशाली लोग थे
जिन्होने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया।
5-3 ग्रामीण समाज में विभिन्नताएँ
यद्यपि खेती की इन नयी तकनीकों से उपज तो बढ़ी लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस
बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा
था। कहानियों में विशेषकर बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े-बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है।
पालि भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था।
बड़े-बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे जो प्राय: किसानों पर
नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय: वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम
साहित्य में भी गाँवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेल्लालर या बड़े जमींदार हलवाहा या उल्वर और दास
अणिमई । यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नयी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी
परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया जिसकी चर्चा प्राय: विध
ग्रंथों में की जाती थी।
5-4 भूमिदान और नए संभ्रात ग्रामीण
ईसवी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का
उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे लेकिन
अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे जिन्हें संभवत: उन लोगों को प्रमाण रूप में
दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर
धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कॄत में थे।
विशेषकर सातवीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कॄत में हैं और कुछ
तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार
करें। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ;लगभग 375-415 ई-पू-द्ध की पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक
परिवार में हुआ था जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कॄत धर्मशास्त्रों के अनुसार, महिलाओं को भूमि जैसी संपत्त पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था
लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी
किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है, क्योंकि वह एक रानी ;आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एकद्ध थी
और इसीलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को
हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का
भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके
प्रतिनिधयों को कई प्रकार की वस्तुएँ प्रदान करते थे।
अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गाँव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता
था और संभवत: अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के
कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में
अंतर है : कहीं-कहीं छोटे-छोटे टुकड़े, तो कहीं कहीं बड़े-बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही
भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन
मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद-विवाद का विषय बना हुआ
है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कॄषि को नए क्षेत्रों
में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक
प्रभुत्व का संकेत मिलता है अर्थात् राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो
उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी
मानना है कि राजा स्वयं को उत्कॄष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते
थे ;जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा है। उनका नियंत्रण ढीला
होता जा रहा था इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। भूमिदान के
प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झाँकी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे
भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था: जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार ;घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वालेद्ध और जगह-जगह घूम कर खेती करने
वाले लोग। सामान्यत: ऐसे लोग अपने जीवन और आदान-प्रदान के विवरण नहीं रखते थे।
6- नगर एव व्यापार
6-1 नए नगर
आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग छठी शताब्दी ई-पू- में उपमहाद्वीप
के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थे। प्राय:
सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के
किनारे बसे थे। उज्जयिनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा
पुहार जैसे नगर समुद्रतट पर थे, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर
व्यावसायिक, सांस्कॄतिक
और राजनीतिक गतिविधयों के जीवंत क्रेंद्र थे।
6-2 नगरीय जनसंख्या :
संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार
हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से
अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं ;हड़प्पा शहरों से भिन्न। लेकिन फ़िर भी यहाँ से विभिन्न
प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कॄष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और
थालियाँ मिली हैं जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कॄष्ण माख्रजत पात्र
कहा जाता है। संभवत: इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने चाँदी, कांस्य, ताँबे, हाथी दाँत, शीशे जैसे तरह-तरह के पदार्थो के बने गहने,उपकरण, हथियार, बतर्न , सीप आरै पक्की मिट्टी मिली हैं। द्वितीय शताब्दी ई- आते-आते
हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ-साथ
प्राय: उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धाेबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ाई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं।
कभी-कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी
कहा गया है। ये श्रेणियाँ संभवत: पहले कच्चे माल को खरीदती थींऋ फ़िर उनसे सामान
तैयार कर बाजार में बेच देती थीं। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले
संभ्रांत लोगों की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का
प्रयोग किया हो।
6-3 उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार
छठी शताब्दी ई-पू- से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल
बिछ गया था और कई दिशाओं में फ़ैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भू-मार्ग
थे। समुद्रतट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए, उत्तरी अफ़्रीका, पश्चिम एशिया तक फ़ैल गयाऋ और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन
और दक्षिणपूर्व एशिया तक फ़ैल गया था। शासकों ने प्राय: इन मार्गों पर नियंत्रण
करने की कोशिश की और संभवत: वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे
धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल पेफरी लगाने वाले
व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े-खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले
व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे जो खतरनाक तो थी, लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मसत्थुवन और
प्रांत में सत्थवाह और सेट्ठी के नाम से प्रसिद्ध सफ़ल व्यापारी बड़े धनी हो जाते
थे। नमक,
अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी-बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे
स्थान तक पहुँचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी-बूटियों की भारी माँग थी। इन
सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुँचाया जाता था।
6-4 सिक्के और राजा
व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चाँदी
और ताँबे के आहत सिक्के ;छठी
शताब्दी ई-पू सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के
दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्राशास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों
का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आहत
सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से
मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी
किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए
हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के ंहंद-यूनानी शासकों ने
जारी किए थे जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ई-पू- में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर
क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी
ईसवी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों
तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिलकुल समान थे। उत्तर और
मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक
प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्र में वस्तुओं का विनिमय
किया जाता था। इसके अलावा, दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं जिनसे
यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बँधा नहीं था क्योंकि दक्षिण
भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य
से संबंधत था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के यौधेय ;प्रथम शताब्दी ई- कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए
थे। पुराविदों को यौधेय शासकों के जारी ताँबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले
हैं जिनसे यौधेयों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के
सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए।
इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से
दूर देशों से व्यापार-विनिमय करने में आसानी होती थी जिससे शासकों को भी लाभ होता
था। छठी शताब्दी ई- से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता
है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन
साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें
दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है, कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय
होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो
कम हो गया लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। क्या इसका
अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते
क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था।
अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे
में अध्ययन कर रहे थे। लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर
क्या लिखा है? ब्राह्मी
लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है अट्ठारहवीं
सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और
देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की
प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले
विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कॄत में लिखे हैं जबकि प्राचीनतम
अभिलेख वस्तुत: प्राप्त में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक
परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ई- में अर्थ निकाल लिया।
7-2 खरोष्ठी लिपि को केसे पढ़ा गया?
पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग
है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद-यूनानी राजाओं लगभग द्वितीय-प्रथम शताब्दी
ई-पू-द्ध द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन
सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने
वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर, दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक, मान लीजिए ‘अ’ प्रयुक्त किया गया। चूँकि प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की भाषा की
पहचान प्राप्त के रूप में की थी इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया।
7-3 अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य
इतिहासकारों एवं अभिलेखशास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए
आइए अशोक के दो अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख में
शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है। उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधयों का प्रयोग किया
गया है जैसे कि देवानांपिय अर्थात् देवताओं का प्रिय और ‘पियदस्सी’ यानी ‘देखने में सुन्दर’। अशोक
नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधयाँ भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का
परीक्षण करने के बाद अभिलेखशास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपिविज्ञान सबमें समानता है, अत: वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक
ने बनवाया था। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे
पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले
के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य
सही है?
इतिहासकारों को बार-बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण
करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके जो उनमें लिखा है, वह सत्य है, संभव है या फ़िर अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्या आपने ध्यान दिया
कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्राय: वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए
ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए।
इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के
किनारे और नगरों के पास प्राकॄतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे, तो क्या वहाँ से आने-जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस
स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्राय: पढ़े-लिखे नहीं थे।
क्या पाटलिपुत्र में युक्त प्राप्त उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते
थे?
क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं हैं। इनमें से
कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं जिसकी व्याख्या प्राय:
अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी
मनोवृत्त में परिवर्तन को भी दर्शाता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते
हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से
प्राप्त हुए हैं लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला
है अर्थात् यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई
थी। इसका हम क्या अर्थ लगाएँ? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी
दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह न सका।
8- अभिलेखीय साक्ष्य की सीमा
अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती
है। कभी-कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है: अक्षरों को हलके ढंग से उत्कीर्ण किया जाता
है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही, अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं।
इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान
हो पाना सदैव सरल नहीं होता क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधत
होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोधपत्रों को पढ़ें ;इसमें से कुछ का उल्लेख काल रेखा में किया गया है तो आप पाएँगे कि विद्वान इनके
पढ़ने की वैकल्पिक विधयों पर चर्चा करते रहते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त
हुए हैं लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके
अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में
सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं, वह संभवत: कुल अभिलेखों के अंशमात्र हैं।
मौर्योंत्तर काल
Posted by: संपादक- मिथिलेश वामनकर on: अगस्त 16, 2008
In: प्राचीन-भारत 5 Comments
शुंग काल
शुङ्ग वंश मौर्य वंश के पश्चात का राजवंश हैं।
हर्षचरित व पुराणों से पता चलता है कि सेनापति पुष्यमित्र ने अपने अंतिम मौर्य
शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की।पुष्यमित्र का साम्राज्य दक्षिण
में नर्मदा तक फैला हुआ था तथा विदिशा उसके राज्य का एक प्रमुख नगर था। “मालविकाग्निमित्रम’ के अनुसार पुष्यमित्र वे शासन काल में उसका पुत्र
अग्निमित्र विदिशा में गोप्तु (उपराजा) के रुप में शासन का संचालन करता था।
अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन के साथ युद्ध करके विदर्भ के एक बड़े हिस्से
पर अधिकार कर लिया।
सन् ४८ ई. पू. में पुष्यमित्र की मृत्यु हो गयी। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार
इस वंश में कुल १० शासक हुए –
क. पुष्यमित्र
ख. अग्निमित्र
ग. वसुज्येष्ठ
घ. वसुमित्र
ड़. अंध्रक (ओद्रक)
च. पुलिद्वक
छ. घोष
ज. वज्रमित्र
झ. भागभद्र और
ट. देवभूति।
इन सबने मिलकर ११२ वर्ष तक राज्य किये।अग्निमित्र के उत्तराधिकारियों के संबंध
में विशेष रुप से कुछ ज्ञात नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पाँचवें
शासक ओद्रक (अंधक) व नौंवे शासक भागभद्र के विदिशा में राजनीतिक गतिविधियों का
साक्ष्य मिलता है। कहा जाता है कि नौवें शासक भागभद्र का संबंध विदिशा स्थित गरुड़
स्तंभ से है, जिसे
स्थानीय लोग खानबाबा (खम्भबाबा) के नाम से पुकारते है। यहाँ उत्कीर्ण लेख के
अनुसार यूनानी शासक अंतलिकित ने अपने राजदूत हेलियोदोरस को भारतीय नरेश भागभ्रद की
राजसभा में राजदूत के रुप में भेजा था। विदिशा में रहते हुए हेलियोदोरस भागवत धर्म
का अनुयायी बन गया तथा विष्णु मंदिर के सम्मुख एक गरुड़- स्तंभ का निर्माण करवाया।
अभिलेखित साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पुष्यमित्र शुंग के
उत्तराधिकारियों का पूर्वी मालवा (विदिशा) क्षेत्र पर अधिकार अंत तक बना रहा।
पुराणों के अनुसार अंतिम राजा देवभूमि अति कामुक था। उसके अमात्य कण्ववंशीय
वसुदेव ने उसकी हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की।
सातवाहन काल
पुराणों के अनुसार सिमुक ने पूर्वी मालवा (विदिशा) क्षेत्र में शासन करने वाले
कण्वों तथा शुंगों की शक्ति को समाप्त कर सातवाहन वंश की स्थापना की है। सातवाहन
वंश का सबसे पराक्रमी राजा शातकार्णि प्रथम को माना जाता है। पुराणों में इसकी
चर्चा कृष्ण (कान्ह) के पुत्र के रुप में की गई है, जिनका शासनकाल संभवतः ३७ ई. पू. से २७ ई. पू. था।
गौतमीपुत्र शातकार्णि ने अपने प्रांतों पर विजय कर अपने वंश की लुप्त गौरव को
प्रतिष्ठा दी। साँची के बड़े स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण एक लेख से शातकर्णि के
पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का पता चलता है।
शातकर्णि की मृत्यु के बाद उनकी रानी नागानिका ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के
संरक्षक के रुप में राज्य किया।
पुराणों से प्राप्त वंशावली के अनुसार इस कुल का छठा राजा का नाम भी शातकर्णि
था। विद्वानों ने इसे शातकर्णि द्वितीय के नाम से पुकारा है। उज्जयिनी से मिले “रजोसिरि सतस’ नामांकित सिक्के शातकर्णि द्वितीय के द्वारा ही मुद्रित
सिक्के माने जाते हैं। इस प्रकार शातकर्णि द्वितीय का अवन्ति पर शासनाधिकार सिद्ध
होता है।
गौतमीपुत्र शातकार्णि सातवाहन वंश का सबसे बड़ा व पराक्रमी राजा था। उसके पुत्र
वसिष्ठिपुत्र पुलुमावी के नासिक अभिलेख में उसकी सफलताओं का वर्णन मिलता है। इस
अभिलेख में उसे पुनः सातवाहन वंश की स्थापना करने वाला, क्षत्रियों के दपं और मान का मर्दन करने वाला तथा क्षहरात
वंश का निर्मूलन करने वाला बताया गया है। इनके शासन क्षेत्र की सूची में अनूप
(महिष्मती के आसपास का निभाड़), आकर (पूर्वी मालवा) और अवन्ति (पश्चिम मालवा) भी शामिल है।
सातवाहन वंश का अंतिम प्रतापी नरेश यज्ञरी शातकर्णि था, जिसने १६५ ई. से १९३ ई. तक राज्य किया। उज्जयिनी लक्षण
मुद्रित सिक्कों से उसके उज्जयिनी पर शासन का प्रमाण मिलता है।
शकों का शासनसाधारणतः विद्वानों का मत है कि उज्जयिनी में शकों का शासन लगातार
तब तक चलता रहा, जब तक
की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के समय में मालवा गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित
नहीं हो गया। इस काल के मालवा के इतिहास से संबंधित बहुत कम अभिलेखीय प्रमाण
उपलब्ध होते हैं। अतः हम मुद्राशास्रीय साक्ष्यों पर ही पूर्णरुपेण निर्भर हैं।
शकों की संयुक्त शासन- प्रणाली में यह परंपरा थी कि वरिष्ठ शासक “महाक्षत्रय’ की उपाधि धारण करता था तथा अन्य कनिष्ठ शासक “क्षत्रय’ कहलाते थे। पश्चिमी क्षत्रपों के समय- समय पर मिलते रहे, सिक्कों से ज्ञात होता है कि “महाक्षत्रय- उपाधि’ बीच- बीच में नहीं मिलती है।
पार्थियन नरेशों की सिंधु प्रदेश की विजय के फलस्वरुप पंजाब तथा उत्तर- पश्चिम
सीमांत प्रदेश में शक सत्ता का अंत हो गया और शकों की एक शाखा पश्चिमी भारत में
अपने राज्य की स्थापना की। इसी शाखा से जुड़े राजवंश हैं –
१. क्षहरात वंश
२. कार्दभक वंश।
क्षहरात वंश का प्रथम ज्ञात क्षत्रप क्षहरात भूभक है। मुद्राओं के अध्ययन से
उसके उज्जैन व भिलसा पर अधिकार का प्रमाण मिलता है। क्षहरात वंश का सबसे शक्तिशाली
शासक नहपान हुआ। वह सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र शातकर्णि का समकालीन था। नासिक
अभिलेख से विदित होता है कि गौतमी पुत्र शातकर्णि ने नहपान ने आकर (पूर्वी- मालवा)
तथा अवन्ति (पश्चिमी- मालवा) को छीनकर उन पर अधिकार कर लिया।क्षहरात कुल के समूल
विनाश के पश्चात पश्चिमी भारत में कदिभक- कुल के शकों का आविर्भाव हुआ। चष्टन इन
वंश का प्रथम क्षत्रप था। अंधाऊ अभिलेख से पता चलता है कि चष्टन और उसका पौत्र
रुद्रदामन साथ मिलकर शासन करते थे। टालमी के भूगोल (१४० ई.) पता चलता है कि अवन्ति
या पश्चिम मालवा की राजधानी पर हिमास्टेनीज का अधिकार था। इस आधार पर यह कहा जा
सकता है कि चष्टन ने नहपान द्वारा खोए हुए कुछ प्रदेशों को सातवाहनों से पुनः
जीतकर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई।
चष्टन के बाद उसका पौत्र रुद्रदामन प्रथम क्षत्रप बना। रुद्रदामन प्रथम के
जूनागढ़ अभिलेख (१५० ई.) से विदित होता है कि उसने अपने पितामह के क्षत्रय के रुप
में आकर (पूर्वी मालवा) तथा अवन्ति (पश्चिमी मालवा) को गौतमी पुत्र शातकर्णि व
उसके उत्तराधिकारी को पराजित करके जीता था। उपरोक्त प्रमाण बताते हैं कि रुद्रदामन
प्रथम के शासनकाल में पूर्वी और पश्चिमी मालवा शक साम्राज्य के अभिन्न अंग थे।
रुद्रदामन प्रथम के बाद भी कदिर्भक वंश के शक नरेशों का मालवा से संबंध बना
रहा और वे उज्जयिनी को अपनी राजधानी बनाकर शासन- संचालन करते रहे। भतृदामन का
पुत्र विश्वसेन चष्टन वंश का अंतिम क्षत्रप था। भर्तृदामन और विश्वसेन की मुद्राएँ
गोंदरमऊ सिरोह तथा साँची से प्राप्त हुई है। इन सिक्कों का अधिक संख्या में मिलना
इस बात का संकेत है कि इन्होंने अपने वंश की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया।
चष्टन वंश के पतन के पश्चात शासन करने वाले परवर्ती शक- क्षत्रपों के कुछ
सिक्के व अभिलेख मालवा- क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जिनसे उन राजाओं के शासन- काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है।
इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक रुद्रसिंह द्वितीय (स्वामी जीवदामन का पुत्र) था, जिसके सिक्के (शक संवत २२७- ३०४ ई.) साँची, गोदरमड (सिरोह) आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। रुद्रसिंह
द्वितीय के उत्तराधिकारी यशोदामन द्वितीय (शक संवत ३१६- ३३२), रुद्रदामन द्वितीय, रुदसेन (तृतीय ३४८- ३७८ ई.), सिंहसेन, रुद्रसेन चतुर्थ, सत्यसिं तथा रुद्रसिंह तृतीय था।
रुद्रसेन तृतीय का शासन- काल करीब ३० वर्षों का था। उसके सिक्के आवरा (मंदसौर), गोंदरमऊ (सिरोह) तथा साँची से प्राप्त होते हैं। सिंहसेन से
लेकर वंश के अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय तक काशासन काल लगभग ३८२ ई. से ३८८ ई. तक
रहा। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) ने व्यक्तिगत रुप से शकों के
विरुद्ध पश्चिमी भारत के शक- नरेश रुद्रसिंह तृतीय को परास्त कर पश्चिमी मालवा पर
अधिकार कर लिया तथा अपने पुत्र गोविंद गुप्त को उज्जयिनी का शासक नियुक्त किया।
विदिशा- एरण क्षेत्र में शासन करने वाले एक नये शक वंश का पता चलता है, जिसके शासक श्रीधर वर्मन का एक अभिलेख एरण तथा दूसरा साँची
के निकट कानखेरा से प्राप्त हुआ है। कानखेरा अभिलेख से मालूम पड़ता है कि श्रीधर
वर्मन ने एक सैनिक अधिकारी के रुप में अपने जीवन की शुरुआत की। बाद में वह सामंत
शासक बना तथा आमीरों की शक्ति क्षीण होने पर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। कानखेड़ा
व एरण से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार उसके शासन काल ३३९ ई. ३६६ ई. के मध्य रही
होगी। समुद्रगुप्त ने श्रीधरवर्मन के राज्य पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया।
कुषाण
मथुरा के इतिहास में यहाँ की जनता शक-क्षत्रपों के समय सर्वप्रथम विदेशी
सम्पर्क में आई परन्तु उनकी अपेक्ष उस पर कुषाण शासन का प्रभाव अधिक चिरस्थाई रुप
से पड़ा। इस समय यहाँ के कलाकारों को अपनी जीविक के लिए विदेशीय का ही आश्रय
ढूँढ़ना पड़ा होगा। इन्हीं कारणों से कवि के समान कलाकार की छेंनी में भी कुषाण
प्रभाव झलकने लगा। नवीन संस्कृति नवीन शासक और नवीन परम्पराओं के साथ नवीन विचारों
का प्रार्दुभाव हुआ जिसने एक नवीन कला शैली को जन्म दिया जो ‘मथुरा कला’ ‘कुषाण कला’ इस अर्थ में उन सभी शैलियों का समावेश होगा जो सोवियत
तुर्किस्तान से सारनाथ तक फैले हुए विशाल कुषाण साम्राज्य प्रचलित थी। इस अर्थ
वल्ख की कला, गांधार
की यूनानी बौद्ध कला, सिरकप (तक्षशिला) की कुषाण कला तथा मथुरा की कुषाण कला का बोध होगा।
कुषाण सम्राट कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव का शासन काल माथुरी कला का ‘स्वर्णिम काल’ था। इस समय इस कला शैली न पर्याप्त समृद्धि और पूर्णता
प्राप्त की। यद्यपि यहाँ की परम्परा का मूल ‘भरहूत’ और ‘साची’ की विशुद्ध भारतीय धारा है यथापि इसका अपना महत्व यह है कि
यहाँ प्राचीन पृष्ठभूमि पर नवीन विचारों से प्रेरित कलाकारों की छेनी ने एक ऐसी
शैली को जन्म दिया जो आगे चलकर अपनी विशेषताओं के कारण भारतीय कला की एक स्वतंत्र
और महत्वपूर्ण शैली बन गई। इस कला ने अंकनीय विषयों का चुनाव पूर्ण सहष्णुता के
साथ किया। इसके पुजारियों ने विष्णु, शिव, दुर्गा, कुबेर, सूर्य आदि के साथ-साथ बुद्ध और तीर्थ करों की भी मानव रुप
से अर्चना की। इन कलाकृतियों को निम्नांकित वर्गों में बाँटा जा सकता है -
- जैन तीर्थ कर प्रतिमाएँ
- आयागप
- बुद्ध व बोधिसत्व प्रतिमाएँ
- ब्राहम्मण धर्म की मूर्तियाँ
- यक्ष-यक्षिणी, नाग आदि मूर्तियाँ तथा मदिरापान के द्रव्य
- कथाओं से अंकित शिलाप
- वेदिका स्तम्भ, सूचिकाएँ, तोरण, द्वारस्तम्भ, जातियाँ आदि
- कुषाण शासकों की प्रतिमाएँ
कुषाण कला की विशेषताएँ -
- विविध रुपों में मानव का सफल चित्रण।
- मूर्तियों के अंकन में परिष्कार।
- लम्बी कथाओं के अंकन में नवीनताएँ।
- प्राचीन और नवीन अभिप्रायों की मधुर मिलावट।
- गांधार कला का प्रभाव।
- व्यक्ति विशेष की मूर्तियों का निर्माण।
१. विविध रुपों में मानव का सफल चित्रण
कुषाण काल में मनुष्य और पशुओं के सम्मुख चित्रण की पुरानी परम्परा छोड़ दी गई।
साथ ही साथ मानव शरीर के चित्रण की क्षमता भी बढ़ गई। विशेषत: रमणी के सौंदर्य को
रुप-रुपांतरों में अंकित करने में मथुरा का कलाकार पूर्णत: सफल रहा। स्तन्य की ओर
संकेत करने वाली स्नेहमयी देवी, झुँन-झुँना दिखलाकर बच्चों का मनोरंजन करने वाली माता विविध
प्रकार के अलंकारों से अपने को मण्डित करने वाली युवतियाँ, धनराशि के समान श्याम केशकलाप को निचोड़ते हुए उनके कारण मोर
के मन में उत्सुकता जमाने वाली प्रेमिकाएँ, उन्मुक्त आकाश के नीचे निर्झर स्नान करने वाली मुग्धाएँ, फूलों को चुनने वाली अंगनाए, कलश धारिणी गोपवधू, दीपवाहिका, विदेशी दासी, मधपान से मतवाली वेश्या, दपंण से प्रसाधन करने वाली रमणी आदि अनेकानेक रुपों में
नारी को मथुरा के कलाकारों के द्वारा पूर्ण सफलता के साथ दिखलाया गया।
पुरुषों के चित्रण में भी वे पीछे नहीं थे। धन संग्रह के प्रतीक बड़ी तोंद वाले
कुबेर,
ईरानी वेश में सूर्य, राजकीय वेश में कुषाण दरबारी, विदेशी पहरेदार फीतेदार चप्पल धारण किए सैनिक, भोले-भाले उपासक, विविध प्रकार की पगड़ियाँ बाँधे हुए पुरुष, बहुमूल्य वस्रालंकारों से मण्डित बोधिसत्व आदि छोटे-बड़े
वर्ग के पुरुष और देवता बड़ी ही कुशलता से अंकित किए गए हैं।
२. मूर्तियों के अंकन में परिष्कार
कुषाण काल की मूर्तियाँ शुंग काल के सामना चपटी न होकर गहराई के साथ उकेरी गई
हैं। प्रारम्भिक अवस्था की तुलना में अब आकृतियों की ऊँचाई बढ़ जाती है।१ उसी अनुपात में निम्नकोटी की आकृतियों की ऊँचाई
में भी बुद्धि होती है। मथुरा की प्रारम्भिक कलाकृतियों की स्थूलता और भोड़ापन
कुषाण काल में पहुँचते-पहुँचते है। मांसल और सुडौल शरीर में बदल जाता है वस्रों के
पहनावे में भी सुरुचि की मात्रा बढ़ जाती है। अब उत्तरीय चपटे रुप में नहीं पड़ता
अपितु मोटी घुमावदार रस्सी के रुप में दिखलाई पड़ता है।२ प्रारम्भिक कुषाण काल की मूर्तियों में केवल
बाँया कन्धा ढका रहता है और कमर के ऊपर वाला वस्र का भाग शरीर से सटा हुआ कुछ पारदर्शक
सा रहता है, नीचे
वाले भाग की ओर कुछ अनुपातत: कुछ काम ध्यान दिया गया है। जाँघ और पैरों की बनावट
में एक प्रकार की कढ़ाई दिखलाई पड़ती है।३
कुषाण काल के मध्य में यह दोष हट जाता है और बहुधा मूर्तियाँ एक घुटना
किंचित मोड़कर खड़ी दिखलाई पड़ती हैं।४
इस काल के मूर्ति निर्माण की दूसरी विशेषता मूर्तियों का आगे और पीछे दोनों ओर
से गढ़ा जाता है। इस काल की बहुसंख्यक मूर्तियाँ ऐसी ही हैं। सम्मुख भाग के समान
कलाकार ने प्रष्ठ भाग की ओर भी खूब ध्यान दिया है। इसकी दो पद्धतियाँ थीं, तो पीछे की ओर पीठ पर लहराते हुए केश कलाप, आभरण, उत्तरीय आदि वस्र आदि दिखलाए जाते थे अथवा पशु-पक्षियों से
युक्त वृक्ष अंकित किए जाते थे।५
३. लम्बी कथाओं के अंकन में नवीनताएँ ६
जातक कथाओं के समान अनेक दृश्यों वाली कथाएँ ‘भूर हूत’ तथा ‘सांची’ में भी
अंकित की गई थी, परन्तु
वहाँ पद्धति यह थी कि एक ही चौखट के भीतर अगल-बगल या तले ऊपर कई दृश्यों को
दिखलाया जाता था, पर अब प्रत्येक दृश्य के लिए अलग-अलग चौखट दिये जाने लगे। उदाहरणार्थ मथुरा से
प्राप्त एक द्वारस्तम्भ पर अंकित नंद-सुन्दरी की कथा७ कई चौखटों में इस प्रकार सजाई गई है कि उससे
सम्पूर्ण द्वार स्तम्भ सुशोभित हो सके। चौखटें अलग-अलग होने के कारण उनके भीतर बनी
मूर्तियों के आकार भी सरलता से ऊँचे बनाए जा सके।
४. प्राचीन और नवीन अभिप्रायों की मिलावट
ɬɖ?ɠके
कलाकारों ने परम्परा से चले आने वाले वृक्ष, लता, और पशु-पक्षियों के अभिप्रायों को अपनाते हुए साथ ही अपनी प्रतिभा से देश काल
के अनुरुप नवीन अभिप्रायों का सृजन किया। उसका फल यह हुआ कि मथुरा की कला में
प्रकृति और उसके अनेक रुपों का अंकन मिलता है। यहाँ विविध वृक्ष लताएँ, मगर, मछलियाँ आदि जलचर, मोर,
हंस, तोते,
आदि पक्षी व गिलहरियाँ, बन्दर, हाथी, शरभ, सिंह आदि छोटे-बड़े पशु सभी दिखलाई पड़ते हैं। पुष्पों में यदि केवल कमल और कमल
लता को ही लें तो उसके अनेक रुप दृष्टिगोचर होते हैं। ईहामृग या काल्पनिक
पशु-पक्षियों जैसे-तोते की चोंच वाला मगर, मानव मुख वाला मेंढ़क आदि का भी यहाँ अभाव नहीं है।
कुषाण कालीन कला में दृष्टिगोचर होने वाले अभिप्रायों को दो वर्गों में बाँटा
जा सकता है।८
१. प्राचीन भारतीय पद्धति के अभिप्राय।
२. नवीन अभिप्राय जिनमें से कुछ पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है।
प्रथम प्रकार के अभिप्राय वे हैं जो विशुद्ध रुप से भारतीय हैं और गांधार कला
के सम्पर्क के पूर्व बराबर व्यवछत होते थे, इनमें पशु-पक्षियों के अतिरिक्त दोहरे छत वाल विहार, गवाक्ष, वातायन, वेदिकाएँ, कपि-शीर्ष, कमल, मणि माला, पंच्चवाट्टिका, घण्टावली, हत्थे या पंचाङ्गुलितल, अष्ट मांगलिक चिन्ह यथा पूर्णघट भद्रासन, स्वास्तिक, मीन-युग्म, शराव-सम्पुट, श्रीवत्स, रत्नपात्र, व त्रिरत्न आदि का समावेश होता है।
नवीन अभिप्रायों से तात्पर्य उन अभिप्रायों से है जो गांधार कला के सम्पर्क
में आने के बाद मथुरा की कलाकृतियों में भी अपनाए गए इनमें (CORINTHIAN
FLOWER) भटकटैया का फूल, प्रभामण्डल, मालाधारी यक्ष, अंगूर की लता, मध्य एशिया और ईरानी पद्धति के ताबीज के समान अलंकार आदि की
गणना की जा सकती हैं।
५. गांधार कला का प्रभाव
कुषाणों के शासन काल में उत्तर-पश्चिम भारत में कला की एक नव-शैली विकसित हुई।
यह भारतीय और यूनानी कला का एक मिश्रित रुप था। जिस गांधार प्रदेश में इसका
बोल-बाला रहा, उसी के
आधार पर इसे ‘गांधार
कला’
के नाम से कला जगत पहचाना गया है। एक ही शासन की छत्र छाया
में पनपने के कारण इन शैलियों का परस्पर सम्पर्क में आना स्वाभाविक था, परन्तु दोनो के मूलभूत सिद्धान्त अलग थे। गांधार कला पर
यूनानी कला का गहरा प्रभाव था। वा मानव चित्रण के बहिरंग पक्ष को अधिक महत्व देती
थी। इसके विपरीत भारतीय विचारधारा में पली हुई मथुरा कला भाव पक्ष की ओर बढ़ती चली
जा रही थी। फल यह हुआ कि गांधार कला से मथुरा के कलाकार कुछ सीमित अंश तक प्रभावित
हुए। इनमें उन्होंने न केवल निर्माण सिद्धान्त ही अपनाए, वरन उनकी कुछ कथावस्तुओं को भी मूर्त रुप दैने का प्रयत्न
किया। उदाहरणार्थ यूनानी योद्धा ‘हरक्यूलियस’ का ‘नेमियनसिंह’ के साथ जो युद्ध हुआ था, उस दृश्य का चित्र मथुरा कला में प्राप्त होता है।
तथापि यह भी सत्य है कि मथुरा की सम्पूर्ण कलाकृतियों में यूनानी प्रभाव
दिखलाने वाली प्रतिमाओं की संख्या बड़ी ही अल्प है। इस प्रभाव को सूचित करने वाले
अंश निम्नांकित हैं -
१. बुद्ध और बोधिसत्वों की कुछ मूर्तियाँ जो अधोलिखित विशेषताओं से युक्त हैं
-
(i) अर्थवर्तुलाकार धारियों वाला वस्र, जिससे बहुधा दोनों कंधे और कभी-कभी पूरा शरीर ढका रहता है
(चित्र ४८)।
(ii) मस्तक पर लहरदार बाल।
(iii) नेत्र और होंठ भरे हुए तथा धारदार, विशेषतया ऊपर की पलकें भारी रहती हैं।
२. बुद्ध जीवन को अंकित करने वाले कतिपय दृश्य, जैसे मथुरा संग्रहालय की मूर्ति संख्या ००.एच.१, ००.एच.७, ००.एन.२, ००.एच.११.
३. कला के कुछ नवीन अभिप्राय, जैसे मालाधारी यक्ष, गरुड़, द्राक्षलता आदि।
४. मदिरापन के दृश्य९
गांधार कला की एक सुन्दर नारी की मूर्ति जो ‘हरिति’ डॉ. वी. एस. अग्रवाल उसे कम्बोजीका की प्रतिमा मानते हैं
जिसका नाम सिंहशीर्ष पर अंकित लेख में मिलता है। अत: सिंहशीर्ष और यह गांधार
प्रतिमा मथुरा के एक ही स्थान से अर्थात् सप्तर्षि टीले से मिले थे। ‘कम्बोजिका’ आदि नामों से पहचानी जाती है (चित्र ४३-४४) मथुरा क्षेत्र
से ही प्राप्त हुई है। उसका उल्लेख इस सन्दर्भ में आवश्यक है। संभव है कि गांधार
कला की यह कलाकृति किसी प्रेमी ने यहाँ मंगवाकर स्थापित की है।
६. व्यक्ति विशेष की मूर्तियों का निर्माण
भारतीय कला को मथुरा की यह विशेष देन है। भारतीय कला के इतिहास में यहीं पर
सर्वप्रथम हमें शासकों की लेखों से अभिलिखित मानवीय आकारों में निर्मित प्रतिमाएँ
दिशलाई पड़ती हैं। कुषाण सम्राट ‘वेमकटफिश’, कनिष्क
एवं पूर्ववर्ती शासक चन्दन की मूर्तियाँ ‘माँट’ नामक स्थान से पहले ही मिल चुकी हैं। एक और मूर्ति जो
संभवत: कुषाण सम्राट ‘हुविष्क’ की हो सकती है, इस समय ‘गोकर्णेश्वर’ के नाम से मथुरा में पूजी जाती है। ऐसा लगता है कि कुषाण राजाओं को अपने और
पूर्वजों के प्रतिमा मन्दिर या ‘देवकुल’ बनवाने
की विशेष रुचि थी। इस प्रकार का एक देवकुल मन्दिर या ‘देवकुल’ बनवाने की विशेष रुचि थी। इस प्रकार का एक देवकुल तो ‘भाँट’ में था। इन स्थानों से उपरोक्त लेखांकित मूर्तियों के
अतिरिक्त अन्य राजपुरुषों की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है, किन्तु वे लेख रहित है।
इस संदर्भ में यह भी अंकित करना समीचीन होगा, कि कुषाण सम्राटों का एक और ‘देवकुल’ जिसे वहाँ ‘बागोलांगो’
कहा गया है, अफगानिस्तान के ‘सुर्खकोतल’ नामक स्थान पर था। यहाँ के पुरातात्विक उत्खन्न के पश्चात
इस ‘देवकुल’ की सारी रुपरेखा स्पष्ट हुई है।
टैग: मौर्योंत्तर काल
बौद्ध धर्म
Posted by: संपादक- मिथिलेश वामनकर on: अगस्त 16, 2008
In: प्राचीन-भारत 8 Comments
जीवन परिचय -गौतम बुद्ध
नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु
और देवदह के बीच
नौतनवा स्टेशन से 8 मील
दूर पश्चिम में रुक्मिनदेई नामक स्थान है। वहाँ एक लुम्बिनी नाम का वन था। गौतम
बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले जब कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नैहर देवदह जा रही थीं, तो रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ। तब इनका नाम सिद्धार्थ
रखा गया। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। जन्म के सात दिन बाद ही माँ का देहांत हो
गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन-पालन किया।
सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद् तो पढ़े ही, राजकाज और युद्ध-विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर-कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। बचपन से ही
सिद्धार्थ के मन में करुणा भरी थी। उससे किसी भी प्राणी का दुःख नहीं देखा जाता
था। यह बात इन उदाहरणों से स्पष्ट भी होती है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके
मुँह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई
बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था क्योंकि किसी को
हराना और किसी का दुःखी होना उससे नहीं देखा जाता था।
एक बार की बात है सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल किया
हंस मिला। उसने उसे उठाकर तीर निकाला, सहलाया और पानी पिलाया। उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई
देवदत्त वहाँ आया और कहने लगा कि यह शिकार मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया और कहा
कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे। मैंने इसे बचाया है। अब तुम्हीं बताओ कि इस पर
मारने वाले का हक होना चाहिए कि बचाने वाले का?
देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोदन से इस बात की शिकायत की। शुद्धोदन
ने सिद्धार्थ से कहा कि यह हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते? आखिर तीर तो उसी ने चलाया था? इस पर सिद्धार्थ ने कहा- पिताजी! यह तो बताइए कि आकाश में
उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर तीर चलाने का ही उसे क्या अधिकार था? हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था? फिर उसने इस पर तीर क्यों चलाया? क्यों उसने इसे घायल किया? मुझसे इस प्राणी का दुःख देखा नहीं गया। इसलिए मैंने तीर
निकालकर इसकी सेवा की। इसके प्राण बचाए। हक तो इस पर मेरा ही होना चाहिए।
राजा शुद्धोदन को सिद्धार्थ की बात जँच गई। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा
कहना। मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा है। इस पर तुम्हारा ही हक है। शाक्य वंश
में जन्मे सिद्धार्थ का सोलह वर्ष की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के
साथ हुआ। राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के लिए भोग-विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया।
तीन ऋतुओं के लायक तीन सुंदर महल बनवा दिए। वहाँ पर नाच-गान और मनोरंजन की सारी
सामग्री जुटा दी गई। दास-दासी उसकी सेवा में रख दिए गए। पर ये सब चीजें सिद्धार्थ
को संसार में बाँधकर नहीं रख सकीं। विषयों में उसका मन फँसा नहीं रह सका।
सांसारिक दुःख देखकर विचलन : वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर
निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दाँत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे-धीरे काँपता
हुआ वह सड़क पर चल रहा था। कुमार (सिद्धार्थ) ने अपने सारथी सौम्य से पूछा- ‘यह कौन पुरुष है? इसके बाल भी औरों के समान नहीं हैं!’
सौम्य ने कहा- ‘कुमार!
यह भी एक दिन सुंदर नौजवान था। इसके भी बाल काले थे। इसका भी शरीर स्वस्थ था। पर
अब जरा ने, बुढ़ापे
ने इसे दबा रखा है।’ कुमार बोला- ‘सौम्य!
यह जरा क्या सभी को दबाती है या केवल इसी को उसने दबाया है?’ सौम्य ने कहा- ‘कुमार, जरा सभी को दबाती है। एक दिन सभी की जवानी चली जाती है!’ ‘सौम्य, क्या किसी दिन मेरा भी यही हाल होगा?’
‘अवश्य, कुमार!’ कुमार कहने लगा- ‘धिक्कार है उस जन्म पर, जिसने मनुष्य का ऐसा रूप बना दिया है। धिक्कार है यहाँ जन्म
लेने वाले को!’
कुमार का मन खिन्न हो गया। वह जल्दी ही लौट पड़ा। राजा को पता लगा, तो उन्होंने कुमार के लिए और अधिक मनोरंजन के सामान जुटा
दिए। महल के चारों ओर पहरा बैठा दिया कि फिर कभी ऐसा कोई खराब दृश्य कुमार न देख
पाएँ। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला, तो उसकी आँखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी साँस तेजी से चल
रही थी। कंधे ढीले पड़ गए थे। बाँहें सूख गई थीं। पेट फूल गया था। चेहरा पीला पड़
गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। फिर कुमार ने सारथी से
पूछा- ‘यह कौन है सौम्य?’
‘यह बीमार है कुमार! इसे ज्वर आता है।’ ‘यह बीमारी कैसी होती है, सौम्य?’ ‘बीमारी होती है धातु के प्रकोप से।’ ‘क्या मेरा शरीर भी ऐसा ही होगा सौम्य?’
‘क्यों नहीं कुमार? शरीरं व्याधिमंदिरम्। शरीर है, तो रोग होगा ही!’ कुमार को फिर एक धक्का लगा। वह बोला- ‘यदि स्वास्थ्य सपना है, तो कौन भोग कर सकता है शरीर के सुख और आनंद का? लौटा ले चलो रथ सौम्य।’ कुमार फिर दुःखी होकर महल को लौट आया। पिता ने पहरा और कड़ा
कर दिया।
फिर एक दिन कुमार बगीचे की सैर को निकला। अबकी बार एक अर्थी उसकी आँखों के
सामने से गुजरी। चार आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे-पीछे बहुत से लोग थे। कोई
रो रहा था, कोई
छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था।
यह सब देखकर कुमार ने सौम्य से पूछा- ‘यह सजा-सजाया, बँधा-बँधाया, कौन आदमी लेटा जा रहा है बाँस के इस खटोले पर?’
सौम्य बोला- ‘यह
आदमी लेटा नहीं है कुमार। यह मर गया है। यह मृत है, मुर्दा है। अपने सगे-संबंधियों से यह दूर चला गया। वहाँ से
अब कभी नहीं लौटेगा। इसमें अब जान नहीं रह गई। घरवाले नहीं चाहते, फिर भी वे इसे सदा के लिए छोड़ने जा रहे हैं कुमार।’ ‘क्या किसी दिन मेरा भी यही हाल होगा, सौम्य?’ ‘हाँ, कुमार! जो पैदा होता है, वह एक दिन मरता ही है।’ ‘धिक्कार है जवानी को, जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है स्वास्थ्य को, जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है जीवन को, जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी सौम्य?’
‘हाँ कुमार!’ ‘कुमार को गहरा धक्का लगा। वह उदास होकर महल को लौट पड़ा।’ राजा ने कुमार की विरक्ति का हाल सुनकर उसके चारों ओर बहुत
सी सुंदरियाँ तैनात कर दीं। वे कुमार का मन लुभाने की तरह-तरह से कोशिश करने लगीं, पर कुमार पर कोई असर नहीं हुआ। अपने साथी उदायी से उसने
कहा- ‘स्त्रियों का यह रूप कभी टिकने वाला है क्या? क्या रखा है इसमें?’ चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला, तो उसे एक संन्यासी दिखाई पड़ा। उसने फिर पूछा- ‘कौन है यह, सौम्य?’ ‘यह संन्यासी है कुमार!’
‘यह शांत है, गंभीर है। इसका मस्तक मुंडा हुआ है। अपने हाथों में
भिक्षा-पात्र लिए है। कपड़े इसके रंगे हुए हैं। क्या करता है यह सौम्य?’
‘कुमार इसने संसार का त्याग कर दिया है। तृष्णा का त्याग कर
दिया है। कामनाओं का त्याग कर दिया है। द्वेष का त्याग कर दिया है। यह भीख माँगकर
खाता है। संसार से इसे कुछ लेना-देना नहीं।’
कुमार को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका चेहरा खिल उठा। बगीचे में पहुँचा, तो हरकारे ने आकर कहा- ‘भगवन पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ है।’
‘राहुल पैदा हुआ!’ -कुमार के मुख से निकला। उसने सोचा कि एक बंधन और बढ़ा। पिता
ने सुना तो पोते का नाम ही ‘राहुल’ रख
दिया!
बुद्ध की तपस्या
सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुँहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ
तपस्या के लिए चल पड़ा। वह राजगृह पहुँचा। वहाँ उसने भिक्षा माँगी। सिद्धार्थ
घूमते-घूमते आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचा। उनसे उसने योग-साधना
सीखी। समाधि लगाना सीखा। पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुँचा और वहाँ
पर तरह-तरह से तपस्या करने लगा।
सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल-चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर काँटा हो
गया। छः साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई।
शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग : एक दिन कुछ स्त्रियाँ किसी नगर से लौटती
हुई वहाँ से निकलीं, जहाँ सिद्धार्थ तपस्या कर रहा था। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा- ‘वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका
सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएँ।’ बात सिद्धार्थ को जँच गई। वह मान गया कि नियमित आहार-विहार
से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए
मध्यम मार्ग ही ठीक होता है।
सुजाता की खीर और बुद्ध को बोध-प्राप्ति : वैशाखी पूर्णिमा की बात है। सुजाता
नाम की स्त्री को पुत्र हुआ। उसने बेटे के लिए एक वटवृक्ष की मनौती मानी थी। वह
मनौती पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुँची। सिद्धार्थ
वहाँ बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्षदेवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर
धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा- ‘जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, उसी तरह आपकी भी हो।’
उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ।
तभी से वे बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ, उसका नाम है बोधिवृक्ष। जिस स्थान की यह घटना है, वह है बोधगया। ईसा के 528 साल पहले की घटना है, जब सिद्धार्थ 35 साल का युवक था। बुद्ध भगवान 4 सप्ताह तक वहीं बोधिवृक्ष के नीचे रहे। वे धर्म के स्वरूप
का चिंतन करते रहे। इसके बाद वे धर्म का उपदेश करने निकल पड़े।
बुद्ध का धर्म-चक्र-प्रवर्तन : जब सिद्धार्थ को सच्चे बोध की प्राप्ति हुई उसी
वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध काशी के पास मृगदाव (वर्तमान में सारनाथ)
पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग
अपनाने के लिए लोगों से कहा। दुःख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। अहिंसा
पर बड़ा जोर दिया। यज्ञ और पशु-बलि की निंदा की।
80 वर्ष की उम्र तक भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का सीधी सरल
लोकभाषा में पाली में प्रचार किया। उनकी सच्ची सीधी बातें जनमानस को स्पर्श करती
थीं। लोग आकर उनसे दीक्षा लेने लगे।
बौद्ध धर्म सबके लिए खुला था। उसमें हर आदमी का स्वागत था। ब्राह्मण हो या
चांडाल,
पापी हो या पुण्यात्मा, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी सबके लिए उनका दरवाजा खुला था।
जात-पाँत,
ऊँच-नीच का कोई भेद-भाव नहीं था उनके यहाँ।
बौद्ध संघ की स्थापना : बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने
लगी। बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। शुद्धोदन और राहुल ने भी
बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जब भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी तो बौद्ध संघ की
स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले
लेने के लिए अनुमति दे दी, यद्यपि इसे उन्होंने विशेष अच्छा नहीं माना।
बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार : भगवान बुद्ध ने ‘बहुजन हिताय’ लोककल्याण के लिए अपने धर्म का देश-विदेश में प्रचार करने
के लिए भिक्षुओं को इधर-उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म
के प्रचार में अपनी अहम् भूमिका निभाई। आज भी बौद्ध धर्म का भारत से अधिक विदेशों
में प्रचार है। चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका आदि में बौद्ध धर्म आज भी जीवित धर्म है और विश्व
में 50 करोड़ से अधिक लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं।
बुद्ध का निर्वाण : भगवान बुद्ध ने सत्य और अहिंसा, प्रेम और करुणा, सेवा और त्याग से परिपूर्ण जीवन बताया। वैशाखी पूर्णिमा को
उनका जन्म हुआ था, उसी दिन उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ और उसी दिन निर्वाण। ईसा से 483 साल पहले भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।
भगवान बुद्ध का आदर्श जीवन युग-युग तक लोगों को सत्य, प्रेम और करुणा की प्रेरणा देता रहेगा। काश, हम उनके जीवन से, उनके उपदेश से कुछ सीख पाएँ!
बुद्ध धर्म के प्रचारक
आनन्द : ये बुद्ध और देवदत्त के भाई थे और बुद्ध के दस सर्वश्रेष्ठ शिष्यों
में से एक हैं। ये लगातार बीस वर्षों तक बुद्ध की संगत में रहे। इन्हें गुरु का
सर्वप्रिय शिष्य माना जाता था। आनंद को बुद्ध के निर्वाण के पश्चात प्रबोधन
प्राप्त हुआ। वे अपनी स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे।
महाकश्यप : महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे, जो तथागत के नजदीकी शिष्य बन गए थे। इन्होंने प्रथम बौद्ध
अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
रानी खेमा : रानी खेमा सिद्ध धर्मसंघिनी थीं। ये बीमबिसारा की रानी थीं और अति
सुंदर थीं। आगे चलकर खेमा बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका बनीं।
महाप्रजापति : महाप्रजापति बुद्ध की माता महामाया की बहन थीं। इन दोनों ने
राजा शुद्धोदन से शादी की थी। गौतम बुद्ध के जन्म के सात वर्ष पश्चात महामाया की
मृत्यु हो गई। तत्पश्चात महा- प्रजापति ने उनका अपने पुत्र जैसे पालन-पोषण किया।
राजा शुद्धोदन की मृत्यु के बाद बौद्ध मठमें पहली महिला सदस्य के रूप में
महाप्रजापिता को स्थान मिला था।
मिलिंद : मिलिंदा यूनानी राजा थे। ईसा की दूसरी सदी में इनका अफगानिस्तान और
उत्तरी भारत पर राज था। बौद्ध भिक्षु नागसेना ने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी
और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया।
सम्राट अशोक : सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी और अखंड भारत के पहले सम्राट
थे। इन्होंने ईसा पूर्व 207 ईस्वी में मौर्य वंश की शुरुआत की। अशोक ने कई वर्षों की लड़ाई के बाद बौद्ध
धर्म अपनाया था। इसके बाद उन्होंने युद्ध का बहिष्कार किया और शिकार करने पर
पाबंदी लगाई। बौद्ध धर्म का तीसरा अधिवेशन अशोक के राज्यकाल के 17वें साल में संपन्न हुआ। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महिंद
और पुत्री संघमित्रा को धर्मप्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इनके द्वारा श्रीलंका के
राजा देवनामपिया तीस्सा ने बौद्ध धर्म अपनाया और वहाँ ‘महाविहार’ नामक बौद्ध मठ की स्थापना की। यह देश आधुनिक युग में भी
थेरावदा बौद्ध धर्म का गढ़ है।
बौद्ध-दीक्षा का मंत्र
बुद्धं सरणं गच्छामि : मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ।
धम्मं सरणं गच्छामि : मैं धर्म की शरण लेता हूँ।
संघं सरणं गच्छामि : मैं संघ की शरण लेता हूँ।
बौद्ध धर्म क्या है?
यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च सरणं गतो।
चत्तारि अरिय सच्चानि सम्मप्पञ्ञाय पस्सति॥
दुक्खं दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिक्कमं।
अरियं चट्ठगिंकं मग्गं दुक्खूपसमगामिनं॥
एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं।
एतं सरणमागम्म सव्वदुक्खा पमुच्चति॥
बौद्ध धर्म कहता है कि जो आदमी बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में आता है, वह सम्यक् ज्ञान से चार आर्य सत्यों को जान लेता है। ये
आर्य सत्य हैं- दुःख, दुःख का हेतु, दुःख से मुक्ति और दुःख से मुक्ति की ओर ले जाने वाला अष्टांगिक मार्ग। इसी
मार्ग की शरण लेने से कल्याण होकर और मनुष्य सभी दुःखों से छुटकारा पा जाता है।
बौद्ध धर्म के आर्यसत्य-चतुष्टय
बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्य चार हैं :
(1) दुःख
(2) दुःख-समुदाय
(3) दुःख-निरोध
(4) दुःखनिरोध-गामिनी
पहला आर्य सत्य दुःख है। जन्म दुःख है, जरा दुःख है, व्याधि दुःख है, मृत्यु दुःख है, अप्रिय का मिलना दुःख है, प्रिय का बिछुड़ना दुःख है, इच्छित वस्तु का न मिलना दुःख है। यह दुःख नामक आर्य सत्य
परिज्ञेय है। संक्षेप में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, यह पंचोपादान स्कंध (समुदाय) ही दुःख हैं।
दुःख समुदय नाम का दूसरा आर्य सत्य तृष्णा है, जो पुनुर्मवादि दुःख का मूल कारण है। यह तृष्णा राग के साथ
उत्पन्न हुई है। सांसारिक उपभोगों की तृष्णा, स्वर्गलोक में जाने की तृष्णा और आत्महत्या करके संसार से
लुप्त हो जाने की तृष्णा, इन तीन तृष्णाओं से मनुष्य अनेक तरह का पापाचरण करता है और दुःख भोगता है। यह
दुःख समुदाय का आर्य सत्य त्याज्य है।
तीसरा आर्य सत्य दुःखनिरोध है। यह प्रतिसर्गमुक्त और अनालय है। तृष्णा का
निरोध करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है, देहदंड या कामोपभोग से मोक्षलाभ होने का नहीं। यह दुःखनिरोध
नाम का आर्य सत्य साक्षात्करणीय कर्तव्य है।
चौथा आर्य सत्य दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद् है। यह दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद्
नामक आर्य सत्य भावना करने योग्य है। इसी आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं।
वे अष्टांग ये हैं :-
1. सम्यक् दृष्टि, 2. सम्यक् संकल्प, 3. सम्यक् वचन, 4. सम्यक् कर्मांत, 5. सम्यक् आजीव, 6. सम्यक् व्यायाम, 7. सम्यक् स्मृति, 8. सम्यक् समाधि।
दुःख का निरोध इसी अष्टांगिक मार्ग पर चलने से होता है। इस ‘आर्यसत्य’ से मेरे अंतर में चक्षु, ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या और आलोक की उत्पत्ति हुई। जबसे मुझे इन चारों आर्य
सत्यों का यथार्थ सुविशुद्ध ज्ञानदर्शन हुआ मैंने देवलोक में, पमारलोक में, श्रवण जगत और ब्राह्मणीय प्रजा में, देवों और मनुष्यों में यह प्रकट किया कि मुझे अनुत्तर
सम्यक् सम्बोधि प्राप्त हुई और मैं अभिसंबुद्ध हुआ, मेरा चित्त निर्विकार और विमुक्त हो गया और अब मेरा अंतिम
जन्म है।
परिव्राजक को इन दो अंतों (अतिसीमा) का सेवन नहीं करना चाहिए। वे दोनों अंत
कौन हैं?
पहला अंत है काम-वासनाओं में काम-सुख के लिए लिप्त होना। यह
अंत अत्यंतहीन, ग्राम्य, निकृष्टजनों के योग्य, अनार्य्य और अनर्थकारी है। दूसरा अंत है शरीर को दंड देकर
दुःख उठाना। यह भी अनार्यसेवित और अनर्थयुक्त है। इन दोनों अंतों को त्याग कर
मध्यमा प्रतिपदा का मार्ग (अष्टांगिक मार्ग) ग्रहण करना चाहिए। यह मध्यमा प्रतिपदा
चक्षुदायिनी और ज्ञानप्रदायिनी है। इससे उपशम, अभिज्ञान, संबोधन और निर्वाण प्राप्त होता
buddha
buddha
टैग: बौद्ध धर्म
सिंधुघाटी सभ्यता
Posted by: संपादक- मिथिलेश वामनकर on: अगस्त 16, 2008
In: प्राचीन-भारत 15 Comments
कांस्य युग
सिंधु घाटी सभ्यता का विकास ताम्र पाषाण युग में ही हुआ था, पर इसका विकास अपनी समकालीन सभ्यताओं से कहीं अधिक हुआ । इस
काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में 2500 ई.पू. से 1700 ईं पू. के बीच एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई जिसकी नगर
नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी । लोगो को नालियों तथा सड़को के महत्व का
अनुमान था । नगर के सड़क परस्पर समकोण पर काटते थे । नगर आयताकार टुकड़ो में बंट
जाता था । एक सार्वजनिक स्नानागार भी मिला है जो यहां के लोगो के धर्मानुष्ठानों
में नहाने के लिए बनाया गया होगा । लोग आपस में तथा प्राचीन मेसोपोटामिया तथा
फ़ारस से व्यापार भी करते थे ।लोगों का विश्वास प्रतिमा पूजन में था । लिंग पूजा
का भी प्रचलन था पर यह निश्चित नहीं था कि यह हिन्दू संस्कृति का विकास क्रम था या
उससे मिलती जुलती कोई अलग सभ्यता । कुछ विद्वान इसे द्रविड़ सभ्यता मानते हैं तो
कुछ आर्य तो कुछ बाहरी जातियों की सभ्यता ।
सिंधु घाटी सभ्यता(३३००-१७०० ई.पू.) यह हड़प्पा संस्कृति विश्व की प्राचीन नदी
घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे की
घाटियों में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा , चन्हुदडो
,
रन्गपुर् , लोथल् , धौलाविरा , राखीगरी , दैमाबाद , सुत्कन्गेदोर, सुरकोतदा और हड़प्पा में हुआ था। ब्रिटिश काल में हुई
खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत
विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं।
हड़प्पा संस्कृति के स्थल
इसे हड़प्पा संस्कृति इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम 1924 में आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त के हड़प्पा नामक
जगह में इस सभ्यता का बारे में पता चला । इस परिपक्व सभ्यता के केन्द्र-स्थल पंजाब
तथा सिन्ध में था । तत्पश्चात इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की दिशा में हुआ । इस
प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अन्तर्गत पंजाब, सिन्ध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमान्त भाग भी थे।
इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में
बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था । यह सम्पूर्ण
क्षेत्र त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है । इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से
तो बड़ा है ही, प्राचीन
मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है । ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी में
संसार भार में किसी भी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था । अब
तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1000 स्थलों का पता चल चुका है । इनमें से कुछ आरंभिक अवस्था के
हैं तो कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के । परिपक्व अवस्था वाले
कम जगह ही हैं । इनमें से आधे दर्जनों को ही नगर की संज्ञा दी जा सकती है । इनमें
से दो नगर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं – पंजाब का हड़प्पा तथा सिन्ध का मोहें जो दड़ो (शाब्दिक अर्थ
–
प्रेतों का टीला) । दोनो ही स्थल पाकिस्तान में हैं । दोनो
एक दूसरे से 483 किमी
दूर थे और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे । तीसरा नगर मोहें जो दड़ो से 130 किमी दक्षिण में चन्हुदड़ो स्थल पर था तो चौथा नगर गुजरात
के खंभात की खाड़ी के उपर लोथल नामक स्थल पर । इसके अतिरिक्त राजस्थान के उत्तरी
भाग में कालीबंगां (शाब्दिक अर्थ -काले रंग की चूड़ियां) तथा हरियाणा के हिसार
जिले का बनावली । इन सभी स्थलों पर परिपक्व तथा उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन
होते हैं । सुतकागेंडोर तथा सुरकोतड़ा के समुद्रतटीय नगरों में भी इस संस्कृति की
परिपक्व अवस्था दिखाई देती है । इन दोनों की विशेषता है एक एक नगर दुर्ग का होना ।
उत्तर ङड़प्पा अवस्था गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजड़ी स्थलों
पर भी पाई गई है ।
नगर योजना
इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहां की विकसित नगर निर्माण योजना । हड़प्पा
तथा मोहें जो दड़ो दोनो नगरों के अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था
। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के
मकानों में सामान्य लोग रहते थे । इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात ये थी कि ये
जाल की तरह विन्यस्त थे । यानि सड़के एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और नगर अनेक
आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था । ये बात सभी सिन्धु बस्तियों पर लागू होती
थीं चाहे वे छोटी हों या बड़ी । हड़प्पा तथा मोहें जो दड़ो के भवन बड़े होते थे ।
वहां के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहां के शासक मजदूर जुटाने और कर-संग्रह
में परम कुशल थे । ईंटों की बड़ी-बड़ी इमारत देख कर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा
कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे ।
मोहें जो दड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है । यह ईंटो के स्थापत्य का
एक सुन्दर उदाहरण है । यब 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर
चौड़ा और 2.43 मीटर
गहरा है । दोनो सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी हैं । बगल में कपड़े बदलने के
कमरे हैं । स्नानागार का फर्श पकी ईंटों का बना है । पास के कमरे में एक बड़ा सा
कुंआ है जिसका पानी निकाल कर होज़ में डाला जाता था । हौज़ के कोने में एक निर्गम
(Outlet)
है जिससे पानी बहकर नाले में जाता था । ऐसा माना जाता है कि
यह विशाल स्नानागर धर्मानुष्ठान सम्बंधी स्नान के लिए बना होगा जो भारत में
पारंपरिक रूप से धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक रहा है । मोहें जो दड़ो की सबसे
बड़ा संरचना है – अनाज रखने का कोठार, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है । हड़प्पा के दुर्ग में छः कोठार मिले हैं
जो ईंटों के चबूतरे पर दो पांतों में खड़े हैं । हर एक कोठार 15.23 मी. लंबा तथा 6.09 मी. चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछेक मीटर की दूरी पर
है । इन बारह इकाईयों का तलक्षेत्र लगभग 838.125 वर्ग मी. है जो लगभग उतना ही होता है जितना मोहें जोदड़ो
के कोठार का । हड़प्पा के कोठारों के दक्षिण में खुला फर्श है और इसपर दो कतारों
में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए हैं । फर्श की दरारों में गेहूँ और जौ के
दाने मिले हैं । इससे प्रतीत होता है कि इन चबूतरों पर फ़सल की दवनी होती थी ।
हड़प्पा में दो कमरों वाले बैरक भी मिले हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने
थे । कालीबंगां में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे बने हैं जो शायद
कोठारों के लिए बने होंगे । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा
संस्कृति के अभिन्न अंग थे ।
हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय के मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का
ही प्रयोग हुआ था । समकालीन मेसोपेटामिया में पकी ईंटों का प्रयोग मिलता तो है पर
इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिन्धु घाटी सभ्यता में ।
जलनिकासी की व्यवस्था
मोहें जो दड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी । लगभग हर नगर के हर छोटे या
बड़ेमकान में प्रांगण और स्नानागार होता था । कालीबंगां के अनेक घरों में
अपने-अपने कुएं थे । घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता जहां इनके नीचे मोरियां
(नालियां) बनी थीं । अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकीं होती
थीं । सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे भी बने होते थे । सड़कों और मोरियों के
अवशेष बनावली में भी मिले हैं ।
कृषि
आज के मुकाबले सिन्धु प्रदेश पूर्व में बहुत ऊपजाऊ था । ईसा-पूर्व चौथी सदी
में सिकन्दर के एक इतिदासकार ने कहा था कि सिन्ध इस देश के ऊपजाऊ क्षेत्रों में
गिना जाता था । पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहुत थीं जिसके कारण यहां अच्छी
वर्षा होती थी । यहां के वनों से ईंटे पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े
पैमाने पर इस्तेमाल में लाई गई जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया ।
सिन्धु की उर्वरता का एक कारण सिन्धु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी । गांव
की रक्षा के लिए खड़ी पकी ईंट की दीवार इंगित करती है बाढ़ हर साल आती थी । यहां
के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवम्बर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो
देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रील के महीने में गेँहू और जौ की फ़सल काट
लेते थे । यहां कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है लेकिन कालीबंगां की
प्राक्-हड़प्पा सभ्यता के जो कूँट (हलरेखा) मिले हैं उनसे आभास होता है कि
राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे ।
सिन्धु घाटी सभ्यता के लोग गेंहू, जौ, राई,
मटर आदि अनाज पैदा करते थे । वे दो किस्म की गेँहू पैदा
करते थे । बनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है । इसके अलावा वे तिल और सरसों भी
उपजाते थे । सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई । इसी के नाम पर यूनान के लोग इस
सिन्डन (Sindon)
कहने लगे ।
पशुपालन
हड़प्पा योंतो एक कृषि प्रधान संस्कृति थी पर यहां के लोग पशुपालन भी करते थे
। बैल-गाय, भैंस, बकरी, भेंड़ और सूअर पाला जाता था . यहां के लोगों को कूबड़ वाला
सांड विशेष प्रिय था । कुत्ते शुरू से ही पालतू जानवरों में से एक थे । बिल्ली भी
पाली जाती थी । कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान मिले हैं । लोग गधे और
ऊंट भी रखते थे और शायद इनपर बोझा ढोते थे । घोड़े के अस्तित्व के संकेत
मोहेंजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिले एक संदिग्ध मूर्तिका से मिले हैं
। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का ज्ञान था ।
व्यापार
यहां के लोग आपस में पत्थर, धातु शल्क (हड्डी) आदि का व्यापार करते थे । एक बड़े भूभाग
में ढेर सारी सील (मृन्मुद्रा), एकरूप लिपि और मानकीकृत माप तौल के प्रमाण मिले हैं । वे
चक्के से परिचित थे और संभवतः आजकल के इक्के (रथ) जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे ।
ये अफ़ग़ानिस्तान और ईरान (फ़ारस) से व्यापार करते थे । उन्होने उत्तरी
अफ़ग़ानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया जिससे उन्हें व्यापार में
सहूलियत होती थी । बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली हैं जिनसे लगता है
कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार सम्बंध था । मेसोपोटामिया के अभिलेखों में
मेलुहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं साथ ही दो मध्यवर्ती व्यापार केन्द्रों
का भी उल्लेख मिलता है – दलमुन और माकन । दिलमुन की पहचान शायद फ़ारस की खाड़ी के बहरीन के की जा सकती
है ।
राजनैतिक ढांचा
इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानागारों का अस्तित्व और विदेशों से
व्यापारिक संबंध किसी बड़ी राजनैतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा पर इसके पुख्ता
प्रमाण नहीं मिले हैं कि यहां के शासक कैसे थे और शासन प्रणाली का स्वरूप क्या था
।
धर्म
हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं । एक
मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है । विद्वानों के मत में
यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा
होगा । इसलिए मालूम होता है कि यहां के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और
इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस् की ।
लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहां का समाज भी मातृ प्रधान था कि नहीं यह कहना
मुश्किल है । कुछ वैदिक सूक्तों में पृथ्वी माता की स्तुति है, किन्तु उनकों कोई प्रमुखता नहीं दी गई है । कालान्तर में ही
हिन्दू धर्म में मातृदेवी को उच्च स्थान मिला है । ईसा की छठी सदी और उसके बाद से
ही दुर्गा, अम्बा, चंडी आदि देवियों को आराध्य देवियों का स्थान मिला ।
पुरुष देवता
यहां मिले एक सील पर एक पुरुष देवता का चित्र मिला है । उसके सिर पर तीन सींग
है और वह योगी की मुद्रा में पद्मासन में बैठा है । उसके चारों ओर एक हाथी, एक गैंडा और एक बाघ है तथा आसन के नीचे एक भैंसा और पांवों
के पास दो हिरण हैं । इसकी छवि पौराणिक पशुपति महादेव से मिलती है । यहां पर लिंग
पूजा का भी प्रचलन था और कई जगहों पर पत्थरों के बने लिंग तथा योनि पाए गए हैं ।
ऋग्वेद में लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा है ।
यहां के लोग वृक्ष पूजक भी थे । एक मृन्मुद्रा में पीपल की डालों के बीच में
विराजमान देवता चित्रित हैं । इस वृक्, की पूजा आजतक जारी है । पशु-पूजा में भी इनका विश्वास था ।
अपने समकालीन मिस्री सभ्यता के विपरीत सिन्धु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर का
प्रमाण नहीं मिलता है ।
शिल्प और तकनीकी ज्ञान
यद्यपि इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे पर
वे कांसे के निर्माण से भली भींति परिचित थे । तांबे तथा टिन मिलाकर धातुशिल्पी
कांस्य का निर्माण करते थे । हंलांकि यहां दोनो में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा
में उपलब्ध नहीं था । सूती कपड़े भी बुने जाते थे । लोग नाव भी बनाते थे । मुद्रा
निर्माण,
मूर्तिका निर्माण के सात बरतन बनाना भी प्रमुख शिल्प था ।
लिपि
प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहां के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया
था । हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई परन्तु अब तक पढ़ी नहीं जा
सकी है।
माप-तौल
लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी सम्पत्ति का लेखा-जोखा आसान हो गया ।
व्यापार के लिए उन्हें माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होने इसका प्रयोग भी किया ।
बाट के तरह की कई वस्तुए मिली हैं । उनसे पता चलता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों (जैसे – 16, 32, 48, 64,
160, 320, 640, 1280 इत्यादि) का उपयोग
होता था । दिलचस्प बात ये है कि आधुनिक काल तक भारत में 1 रूपया 16 आने का होता था । 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनवां यानि एक किलो में कुल 16 कनवां ।
अवसान
यह सभ्यता मुख्यतः 2500 ई.पू. से 1800 ई.
पू. तक रही । ऐसा आभास होता है कि यह सभ्य्ता अपने अंतिम चरण में ह्वासोन्मुख थी ।
इस समय मकानों में पुरानी ईंटों के प्रयोग कि जानकारी मिलती है । इसके विनाश के
कारणों पर विद्वान एकमत नहीं हैं । सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न
तर्क दिये जाते हैं जैसे:
1.बर्बर आक्रमण
2.जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन
3.बाढ तथा भू-तात्विक परिवर्तन
4.महामारी
5.आर्थिक कारण
ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोइ एक कारण नहीं था बल्कि विभिन्न कारणों
के मेल से ऐसा हुआ ।
टैग: सिंधुघाटी सभ्यता, mp psc itihas










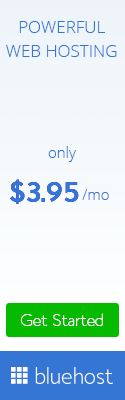




कोई टिप्पणी नहीं:
धन्यवाद